पलाश विश्वास
& भारत मुक्ति मोर्चा संगठन रविवार को कलेक्ट्री परिसर के बाहर बजट की प्रतियां जलाएगा। संयोजक बद्रनाथ भील ने बताया कि मोर्चा के राष्टï्र व्यापी आह्वान पर राष्टï्रीय मूलनिवासी संघ एवं अन्य सामाजिक संगठनों के साथ दोपहर दो से तीन बजे तक कलेक्ट्री पर केंद्रीय बजट की प्रतियां जलाने का कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 से 2011 के लिए जारी बजट में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/एनटी/डीएनटी/अति पिछड़ा वर्ग एवं परिवर्तित मूल निवासी अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं बेरोजगारों के कल्याण की इस बजट में कोई योजना नहीं है। महंगाई कम करने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं, जिसका विरोध किया जा रहा है।
 एक 'ऐतिहासिक ' कदम के तहत ब्रिटेन की संसद समानता कानून में संशोधन करना चाहती है जिसमें जाति आधारित भेदभाव को अवैध घोषित किया जाएगा। हाउस ऑफ लॉर्डस ने इसे मंजूरी दे दी है। विधेयक में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध को शामिल किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ब्रिटेन में व्यापार बढ़ा रही कई भारतीय कंपनियां जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दे रही हैं। BRITAIN NE जाति आधारित भेदभाव को naslvaad ,racial discrimination bataya HAI.HAMAARE YEHAN ENGLISH MEDIA NE TO RACE SHABD KAA USE KIAYA HAI PAR HINDI AKHBARO NE TO KHABAR KO PRINT AUR NET SE BAHAR CHHOD DIYA HAI, BHASKR KI KHABAR ME JATI SYSTEM KO RANGBHED DUNIA MANTI HAI , YEH KHABAR BHI NAHEE HAI. KRIPAYA MERE ENGLISH BLOGS MEI VIVIT KARKE SAREE INFORMATION LEKAR LOGO KO JAAGRUK KARE.
एक 'ऐतिहासिक ' कदम के तहत ब्रिटेन की संसद समानता कानून में संशोधन करना चाहती है जिसमें जाति आधारित भेदभाव को अवैध घोषित किया जाएगा। हाउस ऑफ लॉर्डस ने इसे मंजूरी दे दी है। विधेयक में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध को शामिल किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ब्रिटेन में व्यापार बढ़ा रही कई भारतीय कंपनियां जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दे रही हैं। BRITAIN NE जाति आधारित भेदभाव को naslvaad ,racial discrimination bataya HAI.HAMAARE YEHAN ENGLISH MEDIA NE TO RACE SHABD KAA USE KIAYA HAI PAR HINDI AKHBARO NE TO KHABAR KO PRINT AUR NET SE BAHAR CHHOD DIYA HAI, BHASKR KI KHABAR ME JATI SYSTEM KO RANGBHED DUNIA MANTI HAI , YEH KHABAR BHI NAHEE HAI. KRIPAYA MERE ENGLISH BLOGS MEI VIVIT KARKE SAREE INFORMATION LEKAR LOGO KO JAAGRUK KARE.बाड़मेर & डॉ. भीमराव अंबेडकर ब्लड ग्रुप बाड़मेर का राष्ट्रीय मूल निवासी संघ में विलय हो गया। इसकी घोषणा बामसेफ के संभाग स्तरीय अधिवेशन बालोतरा में अम्बेडकर ब्लड ग्रुप बाड़मेर जिलाध्यक्ष मोतीराम मेणसा ने 50 युवाओं के साथ बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन के समक्ष विलय की घोषणा की। मोतीराम मेणसा ने बताया कि बामसेफ ने देश के मूल निवासियों को व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार कर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी पूरी कर ली है। ऐसी स्थिति में छोटे -छोटे ग्रुप,संगठन बनाकर हमें हमारी सामाजिक ताकत को बंटने नहीं देना चाहिए। वर्तमान में राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से बामसेफ ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए ताकत का निर्माण कर लिया है। हमें हमारे पुरखों की विचारधारा का प्रचार- प्रसार करते हुए आजादी के आंदोलन को सफल बनाना चाहिए।
समानता विधेयक को महारानी की अनुमति मिलने से पहले हाउस ऑफ कॉमंस से अंतिम मंजूरी लेनी होगी। इस नए कानून में विविधता कानून के अलग-अलग तत्वों को एक किया जाना और उम्र के आधार पर भेदभाव को खत्म किया जाना भी शामिल है।
भारतीय कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के अधिकारी जिन्हें नियुक्ति का अधिकार है,उम्मीदवारों से उनके जाति या उपनाम पूछते हैं।
ब्रिटेन स्थित दलित समूहों का अनुमान है कि कम से कम 50,000 दलित ब्रिटेन में निवास करते हैं लेकिन दूसरे अनुमानों के अनुसार यह संख्या 200,000 तक हो सकती है।
मई में होने वाले चुनाव से पहले इसके कानून बनने की उम्मीद है। हाउस आक्र कॉमंस में हाउस ऑफ लॉर्डस के सुझाए गए संशोधनों पर छह अप्रैल को विचार होगा।
हाउस ऑफ लॉर्डस ने जो संशोधन किया है उनमें जाति आधारित भेदभाव को खत्म करना, नौकरी की पेशकश से पहले स्वास्थ्य एवं विकलांगता सूचना मांगने पर प्रतिबंध लगाना और धार्मिक परिसरों में होने वाले असैन्य समारोहों पर प्रतिबंध को हटाना शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासियों के साथ जाति आधारित भेदभाव बढ़ने के प्रमाण सामने आ रहे हैं।
भारतीय मूल के एक ब्रिटिश सांसद ने कहा है कि ब्रिटेन में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए तैयार विधेयक में दक्षिण एशियाई समुदाय के बीच जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने का प्रावधान भी शामिल किया जाना चाहिए।
लंदन में भारतीय मूल के लोगों की बहुलता वाले उपनगर साउथाल से सांसद वीरेंद्र शर्मा ने संसद में समानता विधेयक पर चर्चा के दौरान इस विधेयक को पारित करने का आग्रह किया।
इस विधेयक का उद्देश्य नौ समानता कानूनों को एकीकृत करके एक समानता कानून को अस्तित्व में लाना है। इस कानून में नस्ल,लिंग,विकलांगता,उम्र,धर्म और विश्वास के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव से निपटने के प्रावधान होंगे।
शर्मा ने सरकार से इस सूची में जातिगत भेदभाव पर रोक को भी शमिल करने का आग्रह किया जो ब्रिटेन के दक्षिण एशियाई समुदाय में भारी पैमाने पर विद्यमान है।
शर्मा ने आईएएनएस को एक साक्षात्कार में बताया कि ब्रिटेन और विशेषकर उनके संसदीय क्षेत्र के भारतीय उपमहाद्वीप मूल के बहुत अधिक लोग ब्रिटेन में जातिगत भेदभाव को गैरकानूनी घोषित किया जाना देखना पसंद करेंगे।
शर्मा ने कहा कि विधेयक में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध को शामिल किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ब्रिटेन में व्यापार बढ़ा रही कई भारतीय कंपनियां अनजाने में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दे रही हैं।
शर्मा ने कहा कि भारतीय कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के अधिकारी जिन्हें नियुक्ति का अधिकार है,उम्मीदवारों से उनके जाति या उपनाम पूछते हैं।
ब्रिटेन स्थित दलित समूहों का अनुमान है कि कम से कम 50,000 दलित ब्रिटेन में निवास करते हैं लेकिन दूसरे अनुमानों के अनुसार यह संख्या 200,000 तक हो सकती है।
'वायस ऑफ दलित इंटरनेशनल' की निदेशक एयुजेना क्यूलस ने कहा कि विवाह,नौकरी,सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में जातिगत भेदभाव होता है लेकिन लोग, खासकर दूसरी पीढ़ी के प्रवासी, शर्मिदगी के कारण इस पर चर्चा करने से बचना चाहते हैं।
भास्कर न्यूज & बाड़मेर
भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने रविवार को कलेक्ट्रेट के सामने आम बजट की प्रतियां जलाकर रोष प्रकट किया। भारत मुक्ति मोर्चा के जिला महासचिव मोतीराम मेंणसा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रविवार को कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी करते हुए बजट की प्रतियां जलाई। बजट में एससी,एसटी व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए घोषणा नहीं करने व महंगाई बढऩे का विरोध जताया। इस मौके पर मोतीराम मेंणसा ने कहा कि आम बजट में मूल निवासियों के साथ धोखेबाजी की गई है। बजट में कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर पर्याप्त राशि आबंटित नहीं की गई हैं। इस मौके मोर्चा के प्रताप परमार, श्रवण सेजू, खेतेश कोचरा, हीराराम सेजू, बींजाराम, इन्द्राराम, जगराम, मालाराम, वरिष्ठ कार्यकर्ता रामचन्द्र, प्रकाश, मदनलाल, सुरेश, श्रवण, सुखदेव, तेजाराम, अशोक समेत कई जने मौजूद थे।
बालोतरा & भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर रविवार को आम बजट 2010-11 की प्रतियां जलाई। मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमराराम राठौड़ ने बताया कि आम बजट गरीब व मूल निवासी विरोधी है। यह बजट भारत के पूंजीपतियों के पक्ष का है। इसलिए मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर देशभर में रविवार को आम बजट की प्रतियां जलाई गई।
गडरारोड़ & भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने रविवार को आम बजट की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। मोर्चा के किशोर कुमार जोगू के नेत्तृत्व में उप तहसील मुख्यालय पर आम बजट 2010 की होली जलाई । जोगू ने बताया कि बजट में पूंजीपतियों को शह दी गई हैं। बजट में गरीबों की उपेक्षा की गई है। इस मौके पर कबीराराम, मेघाराम, अर्जुन चौहान, गोपाल, उत्तम लौहार, खेताराम, चौखाराम, किशन वर्मा सहित कई जने मौजूद थे।
भास्कर न्यूज . बाड़मेर
भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से आज रविवार को आम बजट की प्रतिया जला मंहगाई का विरोध किया जाएगा। भारत मुक्ति मोर्चा के जिला महासचिव मोतीराम मेणसा ने बताया कि यह बजट मूल निवासियों के लिए कुठाराघात है। शासक वर्ग ने पूंजीपतियों के साथ मिलकर बजट तैयार किया जो पूंजीपतियों के समर्थन में है। मेणसा ने बताया कि पिछले बजट में 5 लाख 40 हजार करोड़ रुपए देश में मंदी के बावजूद विशेष पैकेज के नाम से पूंजीपतियों को दिया गया। वर्ष 2010-11 के बजट में पहले दिया गया पैकेज वापस न लेकर 4 लाख 18 हजार करोड़ रुपए का विशेष पैकेज फिर से दे दिया। इस बजट में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा र्व के लिए कोई घोषणा नहीं की गई। इसके खिलाफ रविवार को बजट की प्रतियां जलाई जाएगी।
बालोतरा. भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से आम बजट की प्रतियां रविवार को जलाया जाएगा। मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमराराम राठौड़ ने बताया कि यह बजट मूल निवासियों के लिए कुठाराघात है। शासक वर्ग ने पूंजीपतियों के साथ मिलकर बजट तैयार किया है। उन्होंने बताया कि आम बजट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एनटी, डीएनडी, वीजेएनटी, अति पिछड़ा वर्ग, धर्म परिवर्तित मूल निवासी अल्पसंख्यकों के कल्याण विरोधी होने कारण रविवार को देशभर के 20 राज्यों में दो सौ जिलों के 15 हजार कार्यक्रमों के तहत वर्ष 2010-11 के आम बजट की प्रतियां को जलाया जाएगा।
बांसवाड़ा & बामसेफ एवं राष्टï्रीय मूल निवासी संघ की संयुक्त तत्वावधान में रविवार को उपाध्याय पार्क में एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें 14 अप्रैल को डा. भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाने व शहर में वाहन रैली निकाल कर अंबेडकर सर्किल पर सभा आयोजित की जाएगी। इसके लिए ब्लॉक वार कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रतापगढ़ जिले के भरकुंडी माइंस हादसे में मृतक आदिवासी मजदूरों के परिवार वालों को मात्र 20 हजार रुपए देकर पशु के समान मानकर आदिवासियों के साथ अन्याय किया है। संभाग भर में चल रहीं माइंसों में मजदूरों को सुरक्षा एवं भविष्य को लेकर 14 अप्रैल को जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य पाल एवं मुख्य मंत्री को भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट वर्ष 2010-11 को उद्योगपतियों के हित में करके आम जनता के साथ अन्याय किया है। भारत मुक्ति मोर्चा संगठन की नवीन कार्यकारिणी गठित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पंूजीलाल यादव, सोहनलाल पटेल, वालचंद भूरिया, कमल किशोर, लक्ष्मण आदि उपस्थित थे। संचालन रूपलाल बामनिया ने किया व आभार कचरूलाल गरासिया ने माना।
लेम्प्स संचालक मंडल की बैठक : परतापुर। परतापुर लैम्प्स के संचालक मंडल की बैठक अध्यक्ष दिनेश पंड्या की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक मेें खरीफ फसल के लिए खाद की व्यवस्था समय पर उपलब्ध कराने, हरित राजस्थान के तहत पौधारोपण करने के लिए जनजागरण करवाना आदिप्रस्ताव पारित किए गएं। इस अवसर पर उपाध्यक्ष जगदीश पाटीदार, चन्दूलाल जोशी, योगेश जोशी, वेलजी भाई, हीरा भाई ,गमीरा भाई आदि मौजूद थे।
जाति के आधार पर भेदभाव बरता जाना भारत में आम बात है, लेकिन अब इस बात के प्रमाण मिले हैं कि ब्रिटेन में बसे हिन्दू और सिख समुदायों में यह प्रथा जारी है।

उन्होंने यह टिप्पणी तब की जब ब्रिटेन की संसद के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में समान अधिकार वाले विधेयक में संशोधन स्वीकार किया गया। इस विधेयक से जाति के आधार पर भेदभाव बरतना गैर-कानूनी हो जाएगा।
हिन्दू अभियानकर्ता एक लम्बे समय से यह कहते रहे हैं कि ब्रिटेन में बसे एशियाई समुदाय की दूसरी पीढ़ी में भी दलितों को कथित ऊँची जातियों के लोगों के हाथों भेदभाव सहना पड़ता है।
बैरोनेस थॉर्नटन ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को बताया कि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनोमिक एंड सोशल रिसर्च जुलाई या अगस्त में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।
बैरोनेस थॉर्नटन ने कहा, 'हमने जातिगत भेदभाव के प्रमाण जुटाने की कोशिश की है और हमें लगता है कि ऐसे प्रमाण मिल सकते हैं। इसीलिए इस शोध के आदेश दिए गए हैं।'
लिबरल डैमोक्रैट पार्टी के सांसद लॉर्ड एबरी जिन्होंने संशोधन विधेयक पेश किया था कहा कि यह अनुसंधान निर्णायक रूप से यह प्रमाणित कर सकेगा कि जाति के आधार पर भेदभाव होता है।
अगर यह विधेयक कानून की शक्ल लेता है तो हर तरह के छोटे-बड़े संगठन और संस्थाओं को समानता को बढ़ावा देने और कार्यस्थल में भेदभाव रोकने की दिशा में प्रयास करना होगा।
इस समय जो कानून मौजूद है उसमें लिंग, नस्ल, विकलाँगता, यौन झुकाव, धर्म या आस्था, या फिर आयु के आधार पर भेदभाव बरतना गैर कानूनी है। मंत्रियों को आशा है कि इस कानून में और पारदर्शिता लाने से महिलाओं और पुरुषों के वेतन में जो असमानता है उससे निपटने में भी मदद मिलेगी।
नेशनल सैक्युलर सोसायटी के कार्यकारी निदेशक कीथ पोर्टियस का कहना है कि जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव की दिशा में अनुसंधान का निर्णय एक ऐतिहासिक क्षण है।
कीथ पोर्टियस ने कहा, 'जाति के आधार पर भेदभाव का यह अभिशाप जिसमें भारत में लाखों लोगों को अस्पृश्य माना जाता है इस देश में भी चुपचाप चला आया है।'
Caste System is RACIAL Apartheid as UK Bill Links caste to RACE. India Implements MANUSMRITI Afresh with Knowledge Economy Enacted as Right to Education!UK close to banning caste-based discrimination!India rejects bid to include caste in U.N. norms for racial bias!
Indian Holocaust My Father`s Life and Time - THREE HUNDRED Twenty SEVEN
Palash Biswas
http://indianholocaustmyfatherslifeandtime.blogspot.com/
Harriet Harman, minister for women and equality, said: "I'm pleased that the equality bill has completed its third reading in the House of Lords and I want to thank our ministers in the Upper Chamber, Jan Royall and Glenys Thornton, for their hard work and commitment in steering it through to this stage. This is a historic piece of legislation that contains a range of new rights, powers and obligations to help the drive towards equality,... more by Harriet Harman - Mar 24, 2010 - People Management Magazine Online (11 occurrences) |


6-2008 को cryfreedom... पर Palash Biswas
बंगाल में पोंगापंथ
बंगाल के शरतचन्द्रीय बंकिमचन्द्रीय उपन्यासों से हिंदी जगत भली-भांति परिचितहै, जहां कुलीन ब्राह्मण जमींदार परिवारों की गौरवगाथाएं लिपिबद्ध हैं.
महाश्वेता देवी समेत आधुनिक बांग्ला गद्य साहित्य में स्त्राी अस्मिता व उसकी
देहमुक्ति का विमर्श और आदिवासी जीवन यंत्राणा व संघर्षों की सशक्त प्रस्तुति
के बावजूद दलितों की उपस्थिति नगण्य है. हिंदी, मराठी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़ और
तेलुगू भाषाओं की तरह बांग्ला में दलित साहित्य आंदोलन की कोई पहचान नहीं बन
पाई है और न ही कोई महत्त्वपूर्ण दलित आत्मकथा सामने आई है, बेबी हाल्दार के
आलोआंधारि जैसे अपवादों को छोड़कर. आलो आंधारि का भी हिंदी अनुवाद पहले छपा,
मूल बांग्ला आत्मकथा बाद में आयी.
read full story on
http://hashiya.blogspot.com/
Monday, September 28, 2009
जाति समस्या को मानवाधिकार के तहत लाना नामंजूर
-संरा मानवाधिकार परिषद की कोशिश पर भारत ने जताया ऐतराज-नेपाल को भी अपने पाले में लाने की कोशिश करेगा भारतीय खेमा
-कांग्रेस और भाजपा ने भी जताया विरोध
नई दिल्ली
जाति आधारित भेदभाव को मानवाधिकार उल्लंघन के दायरे में लाने की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की कोशिश को भारत से समर्थन मिलने के आसार कतई नहीं हैं। डरबन में 2001 में संरा की ऐसी ही एक कोशिश को परवान चढऩे से रोक चुके भारतीय खेमे ने फिर से अपने प्रयास को तेज कर दिया है। संरा में तैनात भारतीय कूटनीतिकारों ने तो पहले ही इसके विरोध में मुहिम शुरू कर दी है। संरा मानवाधिकार परिषद ने जाति के आधार पर भेदभाव के मामलों को मानवाधिकार उल्लंघन के दायरे में लाने का मन बना लिया है। पिछले दिनों इसके लिए परिषद ने तर्क दिया कि जाति एक ऐसा पहलू है जिसके आधार पर तकरीबन बीस करोड़ लोगों को भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। भारत ने जेनेवा में विश्व की इस ताकतवर संस्था को साफ बता दिया है कि उसके मानवाधिकार परिषद की इस कोशिश से जाति आधारित मुद्दों के अंतरराष्ट्रीयकरण का पूरा खतरा है। उसकी दलील है कि वह जाति आधारित भेदभाव का कड़ाई से विरोध करता है। इसके लिए भारतीय संविधान में हर नागरिक को समानता का अधिकार भी प्राप्त है। आने वाले दिनों में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए सरकार के काबिल कूटनीतिकारों और मानवाधिकार विशेषज्ञों को संरा के साथ बातचीत करने के लिए लगाया जाएगा। जानकारों का मानना है कि भारत को अनुचित तरीके से परेशान करने की ताक में रहने वाले पाकिस्तान जैसे मुल्कों को भी इससे अपने मंसूबों में कामयाब होने का मौका मिलेगा। इस मामले में संरा से सहमत हो रहे अकेले दक्षिण एशियाई मुल्क नेपाल को भी भारत समझाने का प्रयास करेगा। भारत ने यह तर्क भी पेश किया है कि जाति आधारित अन्याय के मामले को अंतरराष्ट्रीय मंच पर तब निपटाया जाना उचित है जब इसका हल तलाशने में किसी भी देश का घरेलू तंत्र पूरी तरफ विफल हो चुका हो। ध्यान रहे यही तर्क भारत ने डरबन में भी दिया था जब जातीय भेदभाव को मानवाधिकार उल्लंघन मानने वाले प्रस्ताव को पारित करने की प्रकिया चल रही थी। भारतीय खेमे का यह भी कहना है कि नस्लीय भेदभाव और जाति आधारित दुव्र्यवहार को अलग-अलग देखने की जरूरत है। बदसलूकी या भेदभाव के अपराधों में दोनों एक-दूसरे से एकदम भिन्न हैं। सरकार के रणनीतिकार मान रहे हैं कि संरा में प्रस्ताव को कानूनी जामा पहना दिए जाने से जाति आधारित अन्याय के मामलों को लेकर अंतरराष्ट्रीय दखल बढऩे का अंदेशा है। कांग्रेस ने भी सरकार को साफ संकेत दिया है कि उसे किसी भी कीमत पर जातिगत भेदभाव के मामलों को मानवाधिकार उल्लंघन के दायरे में लाने की कोशिश पर एतराज है। पार्टी ने कहा है कि भारत में हर नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त है और इसमें कोई बाधा होती है तो उसके लिए घरेलू स्तर पर निपटने के लिए कानून और नियम हैं। कांग्रेस ने कहा है कि विश्व समुदाय के दूसरे देशों में अपना अलग तंत्र है और अलग जातिवादी व्यवस्था है। लिहाजा उन्हें अपनी व्यवस्था भारत पर थोपने का कोई अधिकार नहीं है।
जातीय मामलों को मानवाधिकार से जोडऩे के पक्ष में नहीं है भाजपा
नई दिल्ली
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जातीय मामलों को मानवाधिकार से जोडऩे की मुहिम पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया उभरने लगी है। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने दो टूक कहा है कि इस मामले में भारतीय संविधान एकदम स्पष्ट व पूरी तरह सकारात्मक है और देश में उसी के आधार पर सामाजिक समानता के लिए तमाम कायदे कानून बनाए गए हैैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र का मसौदा समझ से परे है। उसे तो भारत को 'रोल माडलÓ के रूप में स्वीकार करते हुए दुनिया को दिखाना चाहिए कि यहां पर किस तरह समानता के लिए काम किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जातीय मामलों को मानवाधिकार उल्लंघन के तहत शामिल करने की कोशिशों का विरोध करते हुए भाजपा प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि सबसे पहले तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि किन आधारों पर संयुक्त राष्ट्र ऐसा करने जा रहा है। उसकी सोच के पीछे की स्थितियां क्या हैं? दुनिया में जो भी सोच हो, लेकिन भारतीय संविधान इस बारे में बेहद सकारात्मक है और उसमें जातीय समानता लाने के लिए वंचित तबकों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके परिणाम भी सकारात्मक रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव भारत पर थोपा नहीं जाएगा, लेकिन यदि ऐसा किया गया भाजपा इसकी भत्र्सना करेगी और इसका विरोध भी किया जाएगा।
http://workermedia.blogspot.com/2009/09/blog-post_28.html
बहस
मुसलमानों को भूल क्यों जाते हैं
डॉ. असगर अली इंजीनियर
इस साल कांग्रेस अपना 125वां स्थापना दिवस मना रही है. भारत के सभी धर्मो के नागरिकों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जरिए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया परंतु हमारे नेताओं की बहुसंख्यकवादी मानसिकता और स्कूली पाठ्यक्रम तैयार करने वालों के संकीर्ण दृष्टिकोण के चलते, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में अल्पसंख्यकों की भूमिका को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है.
 |
भारत कभी उस अर्थ में राष्ट्र नहीं रहा, जिस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग पश्चिम में किया जाता है. पश्चिमी राष्ट्रों का आधार है एक भाषा और एक संस्कृति. इसके विपरीत, भारत कभी एक भाषा, धर्म या संस्कृति वाला देश नहीं रहा. धार्मिक, भाषायी, नस्लीय और सांस्कृतिक विविधताएं हमेशा से भारत की विशेषता रही हैं. जब हमने ब्रिटिश राज की अपरिमित शक्ति को चुनौती देने का निर्णय किया तभी हमारे नेताओं को यह अहसास हो गया था कि देश के लोगों-विशेषकर हिन्दुओं और मुसलमानों- में एकता कितनी महत्वपूर्ण है. स्वाधीनता संग्राम का एक नारा था, "दीन-धरम हमारा मज़हब, ये ईसाई (अर्थात अंग्रेज) कहां से आए".
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का देश के मुसलमानों ने पूरे उत्साह से स्वागत किया था. इस तथ्य को हमारे इतिहासविदों ने कभी पर्याप्त महत्व नहीं दिया. हमारे इतिहासविद् हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि सर सैय्यद ने मुसलमानों को यह सलाह दी थी कि वे कांग्रेस की सदस्यता न लें. तथ्य यह है कि यह मुस्लिम श्रेष्ठी वर्ग के एक छोटे से हिस्से की राय थी. यह वह तबका था, जिसने 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद अंग्रेजों के हाथों बहुत अत्याचार सहे थे और जो अंग्रेजों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था. हिन्दुओं में भी ऐसे तत्व थे, विशेषकर जमींदारों, राजाओं और महाराजाओं में.
इसके अलावा, सर सैय्यद का कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण शत्रुता का नहीं था. वे तो केवल यह चाहते थे कि मुसलमान आधुनिक शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन पर ज्यादा ध्यान दें. सर सैय्यद की भूमिका के बारे में बहुसंख्यक सांप्रदायिक तत्वों ने कई तरह के भ्रम फैलाए हैं. इस सिलसिले में यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि सर सैय्यद ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए अथक प्रयास किए. उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों को भारत रूपी दुल्हन की दो आँखें निरूपित किया था.
यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सर सैय्यद आम जनता के नेता नहीं थे. वे तो केवल उत्तर भारत के मुस्लिम श्रेष्ठी वर्ग को सामाजिक व शैक्षिक सुधारों के लिए प्रेरित करना चाहते थे. पूरा मुस्लिम श्रेष्ठी वर्ग भी सर सैय्यद के साथ नहीं था. इस वर्ग के एक सदस्य, बम्बई हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बदरुद्दीन तैय्यबजी ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के दौरान अपने 300 साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली थी. वे बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए.
आम मुसलमानों ने कांग्रेस की स्थापना का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और कांग्रेस के सभी आंदोलनों को अपना समर्थन दिया. कांग्रेस के निर्माण से लेकर भारत के स्वतंत्र होने तक, मुसलमान कांग्रेस के साथ बने रहे. इस लेख में हम इसी विषय पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे. सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि किसी समुदाय के कुछ सदस्यों के कामों या गतिविधियों से पूरे समुदाय के संबंध में कोई राय नहीं कायम करना चाहिए. हर व्यक्ति की अपनी प्राथमिकताएं और अपना एजेंडा होता है.
कई लोगों को यह जानकर हैरत होगी कि मुसलमानों में कांग्रेस के सबसे उत्साही समर्थक थे देवबंद के पुरातनपंथी उलेमा. यहां यह जानना भी महत्वपूर्ण होगा कि उलेमा ने सन् 1857 के स्वाधीनता संग्राम में भी भाग लिया था और उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी.
इन उलेमा ने 1857 की क्रांति में बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ दीं और उनमें से सैकड़ो को कालापानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया. कई को इटली के दक्षिण में स्थित माल्टा नामक द्वीप में निर्वासित कर दिया गया. मैंने माल्टा के कब्रिस्तान में सैकड़ो उलेमा की कब्रें देखीं हैं. इन्हें अपने महबूब वतन की मिट्टी में दफन होना भी नसीब नहीं हुआ. जिन उलेमा को निर्वासित किया गया था, उनमें से कई तो बहुत जाने-माने उलेमा थे.
ऐसे ही एक उलेमा थे मौलाना फज़ल काहिराबादी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद दारूल उलूम देवबंद के संस्थापक मौलाना कासिम अहमद नानोटवी- जो स्वयं एक जाने-माने आलिम थे- ने एक फतवा जारी कर मुसलमानों को कांग्रेस की सदस्यता लेने और अंग्रेजों को देश से निकाल बाहर करने के लिए कहा. न केवल यह, उन्होंने इस तरह के एक सौ फतवों को इकट्ठा कर उनका संकलन प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था "नुसरत अल-अहरार" यानी स्वतंत्रता सेनानियों की मदद के लिए. ये उलेमा, आम मुसलमानों के नेता थे और देश से अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेकने के लिए प्रतिबद्ध थे.
एक अन्य जाने-माने आलिम मौलान महमूद उल हसन ने हिन्दुओं और मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह करने का संदेश पूरे देश में फैलाने की एक योजना- जिसे "रेशमी रूमाल षड़यंत्र" कहा जाता है; में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. मौलाना महमूदउल हसन के अलावा अन्य कई उलेमा और आम मुसलमानों ने इस षड़यंत्र में भाग लिया था.
मौलाना हसरत मोहानी एक प्रतिष्ठित उर्दू कवि व बुद्धिजीवी थे. इसके साथ-साथ वे एक महान क्रांतिकारी भी थे, जिन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई में हिस्सा लिया और बहुत कष्ट भोगे. वे बाल गंगाधर तिलक और तिलक के प्रसिद्ध नारे "स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है" के घोर प्रशंसक थे. वे तिलक को "तिलक महाराज" के नाम से पुकारते थे. एक मौलाना होते हुए भी वे सन् 1925 में स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे.
http://raviwar.com/news/307_muslim-freedom-fighters-asgar-ali-engineer.shtml
भूख से किसी की मौत न हो
खाद्यान्न नीति
तरसेम गुजराल
देश भर के राजनीतिज्ञ, ब्यूरोक्रेट, मुख्यधारा के अर्थशास्त्री अचानक नींद से जागते हैं और नींद में चलने वाले किसी मरीज की तरह बड़बड़ाने लगते हैं कि भारत एक बड़ी अर्थशक्ति बनने वाला है। लगभग पैंतालीस रुपये किलो चीनी खरीदकर, सत्तर-पचहत्तर रुपये किलो दाल और सत्रह रुपये आटा खरीदने वाली मजबूर जनता के लिए आर्थिक शक्ति होने के क्या मायने हैं? यह कष्टïों-दिक्कतों के कीच में पैर बचा-बचाकर चलने वाले आम आदमी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। त्रासदी तब और भी भयंकर हो जाती है जब कृषि मंत्री शरद पवार चीनी की बढ़ी कीमतों और कम उपलब्धता को शूगर के मरीजों के लिए बेहतर बताते हैं और दूसरी तरफ उड़ीसा के बालांगीर जि़ले में भूख से मौत की खबर सामने आती है। लोग उपलब्ध आय और बढ़ी हुई कीमतों की रस्सी पर अपने को गिरने से बचाने के लिए सांंस तक रोके हुए हैं और राजनीतिज्ञ इस चिंता से अनजान बेगाने से नजर आते हैं।
राज्य के रेवेन्यू मंत्री ने इस खबर से ही इनकार कर दिया है कि वहां भूख से मृत्यु हुई है। जि़ला क्लेक्टर लोकतांत्रिक राजनीति से अंतरंग नहीं थे, इसलिए कह दिया कि मरने वाले को मृत्यु से पहले दस हज़ार रुपया दे दिया था। मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इस वक्त की मुख्य चिंता गरीबी, भूख से होने वाली मौत या खाद्यान की कमी, किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला नहीं है। कैमरे की आंख और बयान क्रिकेट, फिल्मी हस्तियों, सेक्स-स्कैंडलों और जीवन गति को पीछे ले जाने वाले बाबाओं पर ही केंद्रित है।
हमें देश को बड़ी आर्थिक शक्ति ही नहीं सीधे शब्दों में अमेरिका बनाने का संकल्प दिया जा चुका है। झूठा इंडिया शाइनिंग पहले ही मुंह के बल गिर चुका है। अब तमाम नीतियां कार्पोरेट सेक्टर को केंद्र में रखकर बनाई जा रही हैं। इन नीतियों में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार छोटी-मोटी नौकरी कर पेट पालने वालों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। अर्थव्यवस्था को निभना रुपये के साथ है परंतु ध्यान में डालर है। शशि थरूर कहते हैं भारत प्रतिवर्ष दो खरब डालर की अमीरी प्राप्त कर रहा है। भारत के विदेशी स्रोत एक सौ चालीस बिलियन डालर तक बढ़ गए हैं। लेकिन ध्यान रहे कि देश को इसके लिए अपना सोना लंदन में गिरवी रखना पड़ा है क्योंकि विदेशी विनिमय प्रस्तावों के लिए जरूरी था। संसार के अरबपतियों की सूची में सत्ताइस भारतीय सबसे धनी व्यक्तियाां में हैं जिनमें से अधिसंख्य भारत में हैं और हमारे देश के निर्धन गरीबी रेखा से नीचे गुजर कर रहे हैं। 250 मिलियन भारतीय ऐसी दयनीय स्थितियों में गुजर-बसर करने पर विवश हैं जो हमारे लिए हर तरह से कलंक है। यह स्थिति बहुत गंभीर है।
इसमें दो राय नहीं कि सोवियत संघ के विघटन तथा समाजवाद की जगह पूंजीवादी वर्ग का जीत की खुशी में दमगजे मारना हमारे भविष्य के स्वप्न को भी तोड़-मरोड़ गया। कल्याणकारी राज्य का चेहरा-मोहरा बदल चुका है। सो जनता को सुविधाओं या सहूलियत का हकदार नहीं समझा जाता। बेरोजगारी, अशिक्षा, बीमारी, भूख से बचने के साधन सीमित होते चले गए हैं। गरीबी, भूख, उपेक्षा, शोषण लालगढ़ की परिणतियों तक ले जाता है। पलाश विश्वास ने अपनी डायरी के माध्यम से बताया कि लालगढ़ की समस्या राष्टï्र और राष्टï्र व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्या है। तीन दशकों से कानून व्यवस्था और प्रशासन के काम जहां आदिवासियों को लगातार गरीब बनाए रखते हुए उनकी भुखमरी, बेरोजगारी और लाचारी उनके नियमित विस्थापन की जमीन पर राजनीतिक सत्ता की इमारतें खड़ी की गईं, वे इमारतें माओवादी हिंसा में ढहती नजर आ रही हैं। लोकतंत्र और कानून व्यवस्था, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को इसकी खबर लेनी चाहिए थी। यह भी कहा कि दुनिया का इतिहास गवाह है कि प्रकृति से जुड़े हुए लोग पर्यावरण की पवित्रता की तरह अपनी जीवनशैली और संस्कृति मे हमेशा शांतिपूर्ण बने रहे हैं। परंतु अब वही हथियार उठाने को मजबूर कर दिए गए। विकास का रूप यह है कि बड़े कारखानों के लिए गांव, गांव के लोगों की आजीविका, आदिवासियों के सांस्कृतिक/सामाजिक ढांचे पर गहरा प्रहार किया जाता है। शालबनी में जिंदल के कारखाने के भूमि अधिग्रहण के विरोध में बम विस्फोट हुआ तब से आदिवासी भी माओवादी बना दिए गए।
अब राष्टï्रीय मानवाधिकार कमीशन ने उड़ीसा के मुख्य सचिव से भूख से हुई मौतों पर रिपोर्ट मांगी है। लेकिन क्या भारतीय राजनीतिक ढांचे के व्यवहार में कोई बदलाव आएगा? हमने कालाहांडी, कोरापुर से कोई सबक लिया है? बालांगीर घोरतम निर्धन लोगों का इलाका है जो भारत के सर्वाधिक पिछड़े इलाकों में से एक है। दशाब्दियों से इस इलाके का भाग्य नहीं बदल सका। सरकार की इससे बड़ी असफलता क्या होगी कि आज तक भूख से मौत नहीं रुक पायी। गांधी जी ने हिन्द स्वराज की जो कल्पना की थी उसमें भारत के एक-एक जन तक खुशहाली का हिस्सा पहुंचाने की बात थी। परंतु राज्य के कल्याणकारी नहीं रहने से और आर्थिक शक्ति होने की होड़ में आधारभूत मानवता भी दम तोडऩे लगी है। क्या संतुलन का संबंध सूत्र ढूंढ़ा नहीं जा सकता?
मुद्दा
अ से अमरीका, क से कपिल सिब्बल
देविंदर शर्मा
कुछ साल पहले मुझे लंदन में एक बैठक में आमंत्रित किया गया था, जिसमें विमर्श का मुद्दा था कि इंग्लैंड विकासशील देशों में टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन कैसे दे सकता है. यह बैठक इंग्लैंड के तत्कालीन गृह सचिव हिलेरी बेन द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें करीब 15 लोगों ने भाग लिया था. इंग्लैंड के कई संगठनों ने अन्य विकासशील देशों के साथ-साथ भारत में टिकाऊ कृषि में सहयोग देने संबंधी अनेक प्रस्ताव और परियोजनाएं पेश कीं. इसके बाद हिलेरी बेन ने मुझसे सुझाव मांगे.
 |
मैंने कहा, "मेरी राय में ब्रिटिश कृषि पूरी दुनिया में पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली कृषि व्यवस्था में से एक है. मुझे नहीं लगता कि आपके विश्वविद्यालय और निजी संस्थान इतने काबिल हैं कि वे भारतीय कृषकों और संगठनों को टिकाऊ खेती के बारे में कुछ सिखा सकें."
यह सुनकर हिलेरी बेन चौंक गए और मुझसे पूछा कि इंग्लैंड की कृषि व्यवस्था में सुधार कैसे संभव है. मैंने जवाब दिया, "इंग्लैंड की सरकार को भारतीय किसानों को वहां बुलाना चाहिए, जिन्होंने टिकाऊ खेती व्यवस्था में शानदार प्रदर्शन किया है. और उनसे ही सीखने की कोशिश करनी चाहिए."
कहने की आवश्यकता नहीं है कि बैठक वहीं समाप्त हो गई. इससे पहले कि हम कपिल सिब्बल के तुरही बजाकर विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने की अनुमति देने के मुद्दे पर आएं, मैं आपका ध्यान उस नुकसान की ओर खींचना चाहूंगा, जो आयातित कृषि शिक्षा और अनुसंधान के कारण भारत को उठाना पड़ा है. पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में खोला गया था. इसके बाद से 50 से अधिक कृषि विश्वविद्यालय गठित किए जा चुके हैं.
कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में 50 साल की उपलब्धियों से बेहतर कोई अन्य पहलू नजरिए में परिवर्तन को स्पष्ट नहीं कर सकता. कृषि अनुसंधान व शिक्षा व्यवस्था का ढांचा अमरीका की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया था न कि भारतीय कृषि की समस्याओं को दूर करने के लिहाज से.
हमें बताया गया कि हमारी कृषि निम्न स्तरीय, पिछड़ी और नाकारा है. यह हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है. इन विश्वविद्यालयों में अमरीकी कृषि पर आधारित पाठ्यक्रम होता है. बताया जाता है कि अगर आप भारतीय कृषि को सुधारना चाहते हैं तो अमरीकी कृषि माडल को अपनाना होगा. जबकि हमने अनुभव से सीखा है कि इसी रास्ते पर चलने से हम आज कृषि के सबसे बड़े और गहरे संकट में फंस गए हैं.
ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह सोचते हैं कि अमरीकी कृषि अनुसंधान और शिक्षा व्यवस्था से भारत को बड़ा लाभ हुआ है. मैं इससे इनकार नहीं करता. आखिरकार, हरित क्रांति हुई और इससे देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ. विद्वान इस पर माथापच्ची कर रहे हैं कि हरित क्रांति कितनी सफल रही, किंतु इस तथ्य पर वे विचार नहीं कर रहे हैं कि इसी प्रौद्योगिकी की वजह से वर्तमान कृषि संकट पैदा हुआ है.
चाहे हम स्वीकार करें या न करें, सच्चाई यही है कि यूएस एजेंसी फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट के तहत अमरीका में जिस तरह शिक्षण संस्थान के लिए सरकारी जमीन अनुदान में दी जाती है, ऐसा करने पर भारत में खेतों में अभूतपूर्व खूनखराबा हुआ है. हम नहीं कह सकते कि भारत में जिस तरह की कृषि अनुसंधान और शिक्षा व्यवस्था जारी है, उस पर भयावह कृषि संकट की जिम्मेदारी नहीं है.
आईआईएम और आईआईटी जैसे संस्थानों से पैसा बचाकर कृषि व स्वास्थ्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ केंद्र स्थापित करने में खर्च किया जा सकता है. |
एक देश में, जहां कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया का सबसे विशाल सार्वजनिक ढांचा है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और कृषि को त्यागने पर विवश हैं? अगर कृषि अनुसंधान और शिक्षा में अमरीकी माडल इतना ही अच्छा है तो किसान आज विपत्ति में क्यों हैं और कृषि बर्बादी के कगार पर क्यों पहुंच गई है. एक राष्ट्र के रूप में हमें इसकी पड़ताल करनी चाहिए और पीछे मुड़कर देखना चाहिए. इसमें कुछ बुनियादी गड़बड़ी है.
कृषि, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग या प्रबंधन क्षेत्र कोई भी हो, हमें सिखाया जाता है कि हम जो भी करते हैं, वह निम्न स्तरीय, पिछड़ा और बेकार है. ऐसे में हमारे पास विकास का पश्चिमी माडल अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, यहां तक कि प्रबंधन के क्षेत्र में भी. हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट फार मैनेजमेंट और आईआईटी भी यही कर रहे हैं. ये संस्थान जनता के पैसे से निजी क्षेत्र के लिए छात्रों को शिक्षित करते हैं. मैं अकसर सोचता हूं कि अगर आईआईएम के छात्र को निजी क्षेत्र में ही जाना है तो उद्योग जगत इन संस्थानों को वित्तीय सहायता क्यों नहीं प्रदान करता? इन संस्थानों के वित्तीय पोषण के लिए करदाताओं का पैसा क्यों खर्च होना चाहिए?
भारत में ऐतिहासिक शुचिता की बेहद जरूरत है. आईआईएम और आईआईटी जैसे संस्थानों से पैसा बचाकर कृषि व स्वास्थ्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ केंद्र स्थापित करने में खर्च किया जा सकता है. आयातित जोखिम भरी और गैरजरूरी प्रौद्योगिकी के बजाए कृषि विश्वविद्यालयों की पुनर्संरचना की आवश्यकता है, ताकि ये किसानों के लिए अधिक सार्थक व उपयोगी बन सकें और विद्यमान टिकाऊ प्रौद्योगिकी में सुधार लाया जा सके.
भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह अमरीकापरस्त हैं. वे रहते तो भारत में हैं किंतु सपने अमरीकी देखते हैं. वे भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था में खामियां तलाशते हैं और दोयम दर्जे के अमरीकी, यूरोपीय और आस्ट्रेलियाई कालेज व विश्वविद्यालयों के देश की शिक्षा व्यवस्था पर छा जाने में कुछ गलत नहीं मानते. कोई भी शिक्षा व्यवस्था में सड़न को दूर नहीं करना चाहता. यह सड़न दोयम दर्जे के विदेशी विश्वविद्यालय आयात करने से दूर नहीं होगी. आप एक बुराई को दूसरी बुराई से खत्म नहीं कर सकते.
देश के सामने पहली चुनौती विद्यमान उच्च शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करना है. इसकी शुरुआत शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ शिक्षकों के आकलन की प्रक्रिया में मूलभूत बदलाव लाकर की जा सकती है. साथ ही, पाठ्यक्रम को इस रूप में पुनर्निधारित किया जाना चाहिए कि यह भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके.
हम इसे पसंद करें या न करें, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी शिक्षकों का स्तर भयावह रूप से गिरा हुआ है. कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो अधिकांश उपयुक्त मानदंडों पर खरे नहीं उतरते. उपकुलपतियों का हालत तो और भी दयनीय है. पिछले 15 वर्षो से मैं ऐसे उपकुलपति की तलाश में हूं, जो विश्वास पैदा कर सके. उच्च शिक्षण संस्थानों में इस कदर कमजोर अध्यक्षों के रहते चमत्कार की आशा करना बेमानी है.
कपिल सिब्बल उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण चुनौतियों से कन्नी काट रहे हैं. वह कारपोरेट खेल में शामिल हो गए हैं, जो बी ग्रेड के विदेशी विश्वविद्यालय तक ऐसे छात्रों की पहुंच बनाना चाहता है, जिनके पास पैसा है. हम पहले ही देख रहे हैं कि जो छात्र प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं, वे विदेशी विश्वविद्यालयों का रुख करते हैं.
http://raviwar.com/news/305_a-for-america-k-for-kapilsibbal-devindersharma.shtml
मुद्दा
भुखमरी बढ़ाने की सरकारी तैयारी
सचिन कुमार जैन, भोपाल से
क्या आप यह मानने के लिये तैयार हैं कि जनता की चुनी हुई कोई सरकार अपनी ही जनता को भूख और शोषण का शिकार बनाने के लिये कोई मसौदा तैयार कर सकती है ? अगर नहीं तो कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के सशक्त समूह द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून का जो मसौदा मंत्रिमंडल को विचार और आगे की कार्यवाही के लिए भेजा गया है, उसका एक बार अवलोकन कर लें. इस मसौदे को पढ़ते हुए साफ समझा जा सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून का मसौदा अगर इसी रुप में स्वीकार कर लिया गया तो आने वाले दिनों में देश में भुखमरी, कुपोषण और असमानता अपने चरम स्तर पर पहुँचती नज़र आएगी.
 |
मौजूदा मसौदा कहता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून का लाभ केवल उन गरीब परिवारों को मिलेगा, जिन्हें केंद्र सरकार गरीब मानेगी. लेकिन गरीबी की पहचान और संख्या का आकलन कितना मुश्किल और विसंगतिपूर्ण है, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है. इसके अलावा भारत सरकार साढ़े छह करोड़ परिवारों को गरीब मानती है, जबकि राज्य सरकारें, जो कि हर घर का सर्वे करती हैं और सीधे योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं, उनके मुताबिक 11 करोड़ परिवार ऐसी स्थिति में हैं, जो सबसे वंचित हैं.
आज भी गरीबों की संख्या के इस अंतर को पाटने में सरकार ने कोई रूचि नहीं दिखाई है. प्रस्तावित कानून का मसौदा भी यह कहता है कि इस कानून में राज्य सरकारों द्वारा पहचाने गए गरीबों की इस केन्द्रीय क़ानून में कोई जगह नहीं होगी. यानी साढ़े चार करोड़ परिवारों को खाद्य सुरक्षा का कानूनी हक़ नहीं मिलेगा.
गरीबी, भुखमरी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के जानकार अर्जुन सेनगुप्ता के मुताबिक 77 करोड़ लोग 20 रूपए प्रतिदिन पर गुजारा करते हैं. उत्सा पटनायक के अनुसार 84 करोड़ लोगों को पर्याप्त पोषण युक्त भोजन नहीं मिलता है. मतलब साफ़ है कि जब 75 से 80 फीसदी जनसंख्या भूख के साथ जी रही ह़ो तब इस क़ानून को बीपीएल जैसी काल्पनिक अवधारणा तक सीमित रखने के क्या मतलब हैं.
ताज़ा मसौदे को पढ़ कर साफ समझा जा सकता है कि सरकार की मंशा पोषण और खाद्य सुरक्षा के संबंधों को तोड़ने की दिखती है. वास्तव में न्यूनतम खाद्य अधिकार देने का मतलब है खाद्य असुरक्षा की स्थिति का निर्माण और उसे बनाए रखना. यदि वे लोग, जो कि बीपीएल की सूची के बाहर हैं, परन्तु अपने अस्तित्व के लिए सस्ता राशन चाहते हैं, उन्हें इस व्यवस्था से अनाज पाने का अधिकार होना चाहिए. भोजन का लोकव्यापी अधिकार ही भारत में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है.
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मसौदा एक परिवार के लिए केवल 25 किलो अनाज के अधिकार का प्रावधान करता है, जबकि एक परिवार को कम से कम 56 किलो अनाज, 5 किलो दाल और 4 लीटर खाद्य तेल की जरूरत होती है. भारत में वसा और प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण बहुत बढ़ा है, परन्तु क़ानून में इतनी कम मात्र रख कर हम कुपोषण को कम नहीं कर पायेंगे, यह बाज़ार समर्थक कांग्रेसी सरकार को समझना होगा.
मंत्रियों का समूह यह साफ़ तौर पर मानता है कि खाद्य सुरक्षा की परिभाषा केवल गेहूं और चावल तक ही सीमित रहेगी और इसे किसी भी रूप में प्रस्तावित क़ानून के तहत पोषण सुरक्षा से नहीं जोड़ कर देखा जाएगा. वे यह भी तय कर चुके हैं कि इसके अंतर्गत होने वाले उल्लंघन और अधिकारों के हनन की निगरानी और निराकरण के लिए अलग से प्राधिकरण या आयोग या विशेष अदालतें नहीं बनाई जायेंगी. इसका मतलब यह है कि अधिकारों के हनन की स्थिति में लोगों को वर्तमान न्याय व्यवस्था की शरण में जाना होगा, जहां पहले से ही 3 करोड़, 11 लाख से भी अधिक मुकदमे अपनी सुनवाई और फैसले की प्रतीक्षा में हैं.
मसौदे के अनुसार देश के सभी राज्यों में गरीबी के स्तर को तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेगा, राज्य सरकारें केवल परिवारों की पहचान करके सूची बनाने का ही काम करेंगी, उस संख्या को बढ़ा नहीं सकेंगी. इसका मतलब साफ है कि अधिकारों का दायरा भारत के योजना आयोग द्वारा तय की गई गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए सीमित करके क़ानून की सोच को समग्र तौर पर अनुपयोगी बना दिया गया है.
केंद्र सरकार का यह मसौदा किसी भी स्तर पर राज्य सरकारों को अपनी जरूरत के मुताबिक निर्णय लेने, अधिकारों का विस्तार करने और बेहतर सुरक्षा की कोशिश करने की स्वतंत्रता नहीं देता है. इससे राज्य सरकारों पर अपनी और से संसाधन लगाने का दबाव बढेगा. आज की स्थिति में देखें तो पता चलता है कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को सभी हितग्राहियों को केवल अनाज देने के लिए 1800 करोड़ रूपए अपने राज्य के बजट में से देने पड़ रहे हैं. यदि केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो राज्य सरकारों पर यह भार और बढेगा. आश्चर्य है कि देश के स्तर पर राज्य सरकारें और विपक्षी दल इस मसले का कोई विश्लेषण कर ही नहीं रहे हैं. उनका यह मौन कई लोगों की भूख़ से मौत का कारण बनेगा. शायद यह भी कहा जा सकता है कि सारे राजनीतिक दल भोजन के अधिकार के मामले में बाज़ार के साथ और लोगों के खिलाफ हैं.
आगे पढ़ें
यह उल्लेखनीय है कि भारत में 46 फ़ीसदी बच्चे कुपोषण की गिरफ्त में हैं और यह दर सब-सहारा अफ्रीका से दो गुना ज्यादा है. इतना ही नहीं, यह भी शर्मनाक स्थिति है कि भारत में मातृत्व मृत्यु दर बहुत ऊँची है, जिसका एक बढ़ा कारण महिलाओं में कुपोषण की स्थिति है. ऐसे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लोक व्यापीकरण किये बिना कोई और कदम इस स्थिति में बदलाव नहीं ला सकता है.
देश के हर वयस्क रहवासी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 2 रूपए प्रति किलो की दर से 14 किलोग्राम अनाज, जिसमें ज्वार, बाजरा, जोंधरी सरीखा पोषक अनाज भी शामिल ह़ों, 20 रूपए प्रति किलो की दर से डेढ़ किलो दाल और 35 रूपए प्रति किलो की दर से खाने के तेल की पात्रता ह़ो. बच्चों के सन्दर्भ में यह सुनिश्चित ह़ो कि उन्हें कम से कम आधी मात्रा का अधिकार ह़ो. राशन कार्ड परिवार की महिला मुखिया के नाम पर बनाया जाए. 25 किलो अनाज का प्रावधान असल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किये गए मौजूदा 35 किलो ग्राम अनाज प्रति परिवार के अधिकार से भी कम है. यह एक ऐसा कानून होगा, जो अधिकार देने का वायदा करके वास्तव में मौजूदा अधिकारों को ही सीमित करता है.
जिस दिशा में शरद पवार जैसे मंत्री बढ़ रहे हैं, वहां देश के वृद्द जनों, एकल और विधवा महिलाओं, विकलांगों, छोटे बच्चों, आश्रय विहीनों और गर्भवती महिलाओं की खाद्य सुरक्षा के प्रति कोई संवेदना नज़र नहीं आती है. आज जबकि 46 प्रतिशत बच्चे और 50 फ़ीसदी महिलायें कुपोषण की गिरफ्त में हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु, बाल मृत्यु, मातृत्व मृत्यु भारत में है, दुनिया के कुल भुखमरी के शिकार लोगों में 40 फ़ीसदी भारत में रहते हों, वहां खाद्य सुरक्षा के कानूनी अधिकार को सीमित करने का कुत्सित प्रयास, संविधान का अपमान है और यह साबित करता है कि मौजूदा सरकारें भूख़ और सामाजिक असुरक्षा के शिकार लोगों का नहीं बल्कि मुनाफाखोरों और पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं.
जिस दौर में देश की जीडीपी सबसे तेज़ गति से बढ़ कर 8 और 9 प्रतिशत हुई है, उसी दौर में देश ने भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या में सबसे तेज़ बढ़ोतरी देखी है. बाढ़, सूखा, तूफानों और जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा हुई परिस्थितियों ने भुखमरी को बढ़ाया है, इस बात को नज़रंदाज़ किया जाना लोकतंत्र का अपमान है. सरकार के मंत्रियों द्वारा बार-बार यह कहा जाना कि हम मंहगाई को कम नहीं कर सकते हैं, उनके अपराधी होने का प्रमाण है.
वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिलकुल ध्वस्त होने की कगार पर है. 40 से 60 फ़ीसदी अनाज भ्रष्टाचार की नाली में बह जाता है और नया क़ानून इस व्यवस्था में बुनियादी बदलाव किये बिना फिर इसी तंत्र के हवाले किया जा रहा है. |
पिछले 10 सालों से देश की सबसे बड़ी अदालत भूख़, कुपोषण, सामाजिक असुरक्षा और रोज़गार के मामलों में एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है और अब तक लगभग 65 ऐसे आदेश दे चुकी है, जो सरकार को अपनी जिम्मेदारियों से बांधते हैं, उसे ज्यादा जवाबदेह होने और ज्यादा बजट का आवंटन करने को मजबूर करते हैं.
ऐसे में इस बात पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के वार से बचने के लिए सरकार ने यह क़ानून बनाने का प्रपंच रखा है, उसकी वास्तविक मंशा भूख़ से लड़ने की नहीं है. मध्याह्न भोजन योजना और आंगनबाड़ी में भी खाद्य सुरक्षा के केंद्र हैं परन्तु सरकार इसे कानूनी हक़ के दायरे से बाहर रखने की हर संभव कोशिश कर रही है, ताकि इनमे निजी क्षेत्र को घुसने के अवसर दिए जा सकें.
सर्वोच्च न्यायालय पहले ही अपने आदेशों के जरिए खाद्य सुरक्षा के बहुपक्षीय अधिकारों को सुनिश्चित कर चुका है, जैसे हर परिवार को 35 किलो राशन, वंचित परिवारों के लिए अन्त्योदय अन्न योजना के तहत और सस्ता राशन, शिशुओं और बच्चों के लिए आई सी डी एस के तहत पूरक पोषण आहार, मातृत्व सहायता योजना और जननी सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं को सुरक्षा, स्कूलों में मध्यान भोजन, वृद्धावस्था पेंशन, आश्रय विहीनों, शहरी गरीबों, बेघर बच्चों एकल महिलाओं और 6 वर्ष के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के अधिकार शामिल हैं.
मंत्रियों के सशक्त समूह ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अपर्याप्त अधिकारों को देने और बहिष्कार को बढ़ाने वाला अपना मसौदा ऐसे समय में जारी किया है, जबकि इन अधिकारों का विस्तार करने की अनुशंसा करने वाली वाधवा समिति ने अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को अभी ही सौंपी है. इससे लगता है कि मंत्रियों के सशक्त समूह ने रोटी के अधिकार पर न्यायालय में चल रही कार्यवाही को सुनियोजित तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश की है. वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिलकुल ध्वस्त होने की कगार पर है. 40 से 60 फ़ीसदी अनाज भ्रष्टाचार की नाली में बह जाता है और नया क़ानून इस व्यवस्था में बुनियादी बदलाव किये बिना फिर इसी तंत्र के हवाले किया जा रहा है.
आश्चर्यजनक ये है कि सरकार केवल अनाज के वितरण की ही बात कर रही है, वितरण के लिए अनाज पैदा करने, किसानों के संरक्षण, कंपनियों द्वारा खेती की जमीन, जंगल और पानी के दुरुपयोग को रोकने के कोई संकेत सरकार नहीं दे रही है. इसका मतलब यह है कि जल्द ही अनाज आयात करने की तैयारी ह़ो रही है, ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पंहुचाया जा सके. कोशिश यह भी है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज के बजाये नकद राशि का भुगतान हितग्राहियों को कर दिया जाए, ताकि सरकार को खुद अनाज ना खरीदना पड़े और सब्सिडी पर होने वाला खर्च बच जाए. ऐसे में क्या यह कहना गलत होगा कि सरकार भूख, भुखमरी और शोषण को बढ़ाने की तैयार कर रही है ? इस एक वाक्य को तथ्य के बजाये एक सवाल के रुप में पढ़ने की जरुरत है, जिसके लिये फिलहाल न सरकार तैयार है और न दूसरे राजनीतिक दल.
25.03.2010, 04.40 (GMT+05:30) पर प्रकाशित
Pages:| 1 | 2 |
महात्मा गाँधी के संसदीय लोकतंत्र सम्बन्धी विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता
 यह आम धारणा है कि विश्व में सर्वप्रथम राजतंत्र का जन्म हुआ है और उसका विकसित रूप लोकतंत्र है। किन्तु भारतीय साहित्य और राजनीति में इसके विपरीत प्रमाण मिलते हैं, जिसके अनुसार भारत में सर्वप्रथम लोकतंत्र का जन्म हुआ और राजतंत्र उसका विकृत रूप है। भारत में राजनीतिक विचारधारा देशकाल से प्रभावित होकर पाश्चात्य विचारधारा से बहुत कुछ भिन्न रही है। यद्यपि भारतीय साहित्य में लोकतंत्र में रूचि नहीं रखते थे। वास्तव में उनकी दृष्टि से लोकतंत्र और धर्म मर्यादित राजतंत्र में अधिक अन्तर नहीं था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब लोकतंत्र पर बहस होती है तो उत्तरदायी लोकतंत्र अर्थात संसदीय लोकतंत्र उभर कर हमारे सामने आता है। जिसे यदि सीमित बहुसंख्यक जनता का शासन भी कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा । बहुदलीय प्रणाली, राजनीतिक दल-बदलद्व स्पष्ट बहुमत का आभाव आदि अनेक दोषों से ग्रसित संसदीय लोकतंत्र की सफलता पर विद्वानों में पर्याप्त बहस होने लगी है। भारत के संदर्भ में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी लोकतन्त्र के पक्षधर होते हुए भी संसदीय लोकतन्त्र के प्रति अपनी आपत्तियां रखते है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि गांधीजी के राजनीतिक विचारों में लोकतंत्र के प्रति उनकी निष्ठा सर्वत्र विद्यमान है। किन्तु उन्होंने लोकतंत्र के सामाजिक उत्थान के पक्ष को महत्व दिया है। वे अभिजातीय लोकतंत्र तथा पंचवर्षीय मतदान की प्रणाली वाले औपचारिक लोकतंत्र के पक्ष मे नहीं है। उनके लोकतंत्र में एक ओर समाज के दलित वर्गो द्वारा कुलीन तथा पूंजीपति वर्गो के नियन्त्रण के विरूद्व राजनीतिक आन्दोलन की प्रेरणा मिलती है तो दूसरी ओर ऐसे आर्दश समाज की मांग, जिसमें व्यक्ति को स्वशासन का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके । गाँधीजी के सर्वोदयी उदारवादी लोकतंत्र में दलविहीन राजनीति के दर्शन होते हैं। गाँधीजी सर्वोदय तथा अंत्योदय की दृष्टि से ऐसे समतावादी समाज के समर्थक हैं जिसमें नेता तथा जनता एक ही धरातल पर सादगी एवं संयम से जनसेवा का कार्य करते रहें। वे लोकतंत्र को ''मिलावटविहिन अहिंसा का शासन'' मानते हैं। लोकतंत्र अर्थात् अहिंसा, व्यक्ति की आत्मशुद्वि या नैतिक उत्थान को लिए हुए हैं। राजनीतिक स्वशासन जिसमें अनेक पुरूषों तथा स्त्रियों का स्वाशासन अन्तर्निहित है। व्यक्तिगत स्वशासन से बढकर नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि गाँधीजी को इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि व्यक्तिगत स्वशासन वह शासन है, जो न केवल सामाजिक मूल्यों वरन् व्यक्ति की गरिमा को भी बनाये रखने में सहायक है। गाँधीजी पाश्चात्य देशों के लोकतान्त्रिक उदाहरणों से सन्तुष्ट नहीं है, क्योंकि वहां शस्त्रास्त्र की होड, साम्रज्यबाद, शोषण, पूंजीवाद, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा नेतृत्व के अभाव ने सच्चे लोकतान्त्रिक मूल्यों को भुला दिया है। राज्य का आर्थिक कार्यों में हस्तक्षेप, राज्य शक्ति के बढते हुए दायरे का प्रतीक बन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निगलने के लिये मुँह बाएँ खडा है। ऐसे भयावह राज्य से मुक्ति प्राप्त करने के लिये उचित नियंत्रण तथा सन्तुलन ढूंढने की आवश्यकता हैं। गाँधीजी के विचारों से स्पष्ट होता है कि उनकी नजर में लोकतंत्र समाज के सभी वर्गो के समस्त भौतिक और आध्यात्मिक साधनों को सबकी भलाई के लिये संगठित करने की कला और विज्ञान हैं। उनका मानना है कि लोकतंत्र वह है जिसमें दुर्बल और सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हों लेकिन वे यह भी मानते है कि विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं हैं। गाँधीजी के चिन्तन में लोकतंत्र के प्रति स्वाभाविक निष्ठा प्रकट होती है क्योंकि उनकी विचारधारा में व्यक्ति को जो सम्मान प्राप्त है, वही लोकतंत्र का भी आधार है। सार यह है कि व्यक्ति का सर्वोच्च एवं सर्वागींण विकास गाँधीजी के चिन्तन में प्रमुख स्थान रखता है। यदि लोकतंत्र, शासन अथवा जीवन की वह पद्वति है जो समाज के सभी व्यक्तियों को समानता के धरातल पर संगठित कर उन्हें उनकी सर्वोच्च मंजिल तक पहुँचाती है तो गाँधीजी को यह अत्यन्त प्रिय है लेकिन पश्चिमी प्रजातंत्र अथव संसदीय प्रणाली ऐसा करने में सर्वथा असमर्थ है इसलिए गाँधीजी इसके समर्थक नहीं है। गाँधीजी ने पाश्चात्य राज्य पद्धतियों की आलोचना की । अन्य राज्य पद्धतियां तो दोषपूर्ण पहले से ही मानी जाती थी, परन्तु संसदीय लोकतन्त्र जो सभी राज्य पद्धतियों में निर्दोष माना जाता है तथा मानव-कल्याण और हित का दावा करता है। उनके मत में वह भी दोषपूर्ण है और हिंसा पर आधारित है, इससे मानव का सच्चा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होनें प्रचलित संसदीय लोकतंत्र में अविश्वास व्यक्त किया। लोकतंत्र जिस रूप में पश्चिम में स्वीकृत है उससे वे सहमत नहीं थे। संसदीय लोकतंत्र की उनकी आलोचना का मुख्य आधार यह था कि उसमें ईमानदारी और जन-कल्याण की भावना से बहुत कम काम होता है और ढग तथा प्रदर्शन का अधिक। गाँधीजी का कहना था कि अहिंसा और नैतिक शुद्धता में विश्वास न होने के कारण पश्चिम के राज्यों में नाममात्र का लोकतंत्र है, उनमें लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रति वास्तविक लगाव नहीं पाया जाता है। गाँधीजी प्रेम को लोकतंत्र का सच्चा आधार मानते है, उनके विचार में प्रेम लोकतंत्र के विकास में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसके अलावा स्वयं व्यक्ति का अच्छा होना, अहिंसा व नैतिकता के नियमों का पालन आदि को भी वे लोकतंत्र के विकास में सहायक मानते हैं। गाँधीजी के इन विचारों से उन लोगों को छोडकर जिन्हें लोकतन्त्रिय शासन में विश्वास नहीं है, शायद ही कोई इन्कार कर सकता है। गाँधीजी के विचारों से यह भी स्पष्ट होता है कि पश्चिम में लोकतत्र के सफल न हो सकने का कारण संस्थाओं की पूर्णता उतनी ही है, जितनी सिद्धान्तों की अपूर्णता है। विशेष रूप से हिंसा और असत्य की उपयोगिता म विश्वास । लोकतंत्र उन गलत विचारों और आदर्शो से विकृत होता हैं। जो मनुष्यों का संचालन करते हैं यदि जनता ने शुद्ध अहिंसा के मार्ग को अपनाया तो लोकतंत्रवादी राज्य के ये दोष बहुत कम हो जायेंगे। गाँधीजी ने विश्वास प्रकट किया कि लोकतंत्र का विकास, बल प्रयोग से नहीं हो सकता । लोकतंत्र की सच्ची भावना बहार से नहीं अपितु भीतर से उत्पन्न होती है। कानून पास करने से बुराइयां दूर नहीं की जा सकती, मूल बात तो यह है कि हृदय को बदला जाये । यदि हृदय बदले बिना व्यवस्थापन कर दिया जाये तो महत्वहीन होगा । कानून सदैव आत्मरक्षा के लिये बनाये जाने चाहिए यदि वे उन्नति और विकास को रोकते हैं तो वे बेकार हैं, कोई भी मानवीय कानून स्थायी रूप से व्यक्ति के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकते। गाँधीजी की पुस्तक ''हिन्द-स्वराज्य'' के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वे संसदीय लोकतंत्र के पक्ष में नही थें । उनके मत में - ''जिसे आप पार्लियामेंट की मॉ'' कहते है, वह तो बांझ और वैश्या है। ये दोनों शब्द कठोर हैं पर उस पर पूरी तरह चरिर्ताथ होते है। उसे बांझ मैं इसलिए कहता हूं कि अब तक उसने एक भी अच्छा काम अपने आप नहीं किया। उसकी स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति है कि उसके ऊपर दबाव देने वाला कोई न कोई हो तो वह कुछ भी न करे और वैश्या वह इसलिए है कि जो मन्त्रीमण्डल वह बनाती है उसके वश में रहती है।'' इसके अलावा उसका कोई एक मालिक मुख्तार भी नहीं है। उसका मुखिया कोई एक आदमी हो ही नहीं सकता। उसका मुखिया जब कोई बनता है जैसे कि प्रधानमंत्री, तब भी उसकी चाल एक सी नही रहती। जो दुर्गति वैश्या की होती है वही सदा उसकी रहती है। प्रधानमन्त्री को संसद की चिन्ता अधिक नहीं होती, वह तो अपनी शक्ति के मद में चूर रहता है, उसका पक्ष कैसे जीते इसी की चिन्ता उसे रहती है। संसद ठीक काम कैसे करे इसकी फिक्र उसे ज्यादा नहीं होती। अपने पक्ष का बल बढाने के लिए वह संसद से कैसे कैसे काम करवाता है। गाँाधीजी के से विचार आज के सन्दर्भ में पूर्णतया सत्य प्रतीत होते हैं। प्रायः देखा गया है कि संसदीय प्रजातंत्र में दलगत राजनीति कार्य करती है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं परन्तु वास्तव में उसकी कर्त्तव्यनिष्ठा अपने परिवार या अपनी पार्टी तक ही सीमित रहती है। जनता के कल्याण के लिए वे कुछ भी नहीं कर पाते । जो जिस दल का सदस्य होता है उसी को आँख मूंद कर वोट कर देता है, अथवा देने को मजबूर है। कोई इस नियम का अपवाद बन जाए तो समझ लीजिए कि उसकी सदस्यता के दिन पूरे हो गए। जितना समय और पैसा संसद बरबाद करती है उतना समय और पैसा थोडे से भले आदमियों को सौंप दिया जाय तो उद्वार हो जाय । एक ब्रिटिस संसद सदस्य ने तो यहां तक कह दिया कि संसद इस लायक नहीं रही कि कोई सच्चा ईसाई उसका सदस्य हो सके। एक अन्य सदस्य का कहना था कि संसद तो अभी दूध पीती बच्ची हैं । इस पर बच्चा सदा बच्चा ही बना रहे ये बात क्या आपने देखी है। सात सौ साल हो जाने पर भी संसद बच्ची ही बनी है तो सयानी कब होगी? इसी कारण संसद में बहुत अधिक अस्थिरता पाई जाती है और यही करण है कि उसके फैसलों में कोई पक्कापन नहीं होता । आज का फैसला कल रद्द कर दिया जाता है। सम्भवतः एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि संसद ने कोई काम करके उसे अन्त तक पहुंचाया हो । यही नहीं संसद क सदस्य महत्वपूण्र्ा और बडे मसलों पर विवाद के समय बैठे-बैठे ऊंधा करते है, कभी संसद में वे इतना शोर मचाते हैं कि सुनने वालों की हिम्मत टूट जाती है। भारत की संसद में तो अनेक बार संसद सदस्यों द्वारा गाली-गलौंच छीना-झपटी, एक दूसरे के कपडे फाड देना, माईक व पेपरवेट फेंकना, टेबल उलट देना जैसी घटनाएं देखी गई हैं। जिससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। क्या यही वे सदस्य हैं जो सरकार में हमारे प्रतिनिधी हैं? संक्षेप में संसद न तो किसी के प्रति वफादार होती है और न उसमें सृजन की क्षमता ही होती है। इसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया । गांधीजी के मत में ब्रिटिश प्रजातंत्र में समस्त जनता के कल्याण का भार कुछ चुने हुए प्रतिनिधि ले लेते हैं। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी हाथ नहीं बंटा पाती है। सम्पूर्ण जनता वास्तव में अपने कल्याण के लिए राज्य के प्रतिनिधियों की गुलाम हो जाती है, उनका शोषण होता है। अतः गाँधीजी की राय में यह पद्वति हिंसा से पूर्ण है। उसमें नाजीवाद और फांसीवाद उपनिवेशवादी नीति को ढकने का एक बडा आवरण है। इसकी सभी संस्थाएं अलोकतांत्रिक तथा हिंसा से पूर्ण है। अतः ब्रिटिश लोकतंत्र उपयोगी पद्वति नहीं है। गांधीजी का यह मत कुछ अंशो में सत्य माना जा सकता है। यह सत्य है कि संसद के सदस्य कठोर दलीय अनुशासन में बन्धें होते हैं और उनका सम्पूर्ण व्यहवार अपने अपने दल के नेता के इशारे द्वारा निर्धारित होता है किन्तु गाँधीजी की इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि संसद ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया । भले ही संसद के सदस्य ने जनभावनाओं को अभिव्यक्त कर उसकी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा की है। यह कहना भी सत्य नहीं है कि संसद के सदस्य दलगत राजनीति से प्रेरित और सदैव दलीय नेता के इशारे पर कार्य करते रहे है। ब्रिटेन और भारत में ऐसे अनेक अवसर आये हैं जब संसद के सदस्यों ने दलीय राजनीति से प्रेरित होकर नहीं बल्कि अपने विवेक और अन्तरात्मा की आवाज के आधार पर कार्य किया है। १९७५ में प्रधानमन्त्री स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा लगाये गए आपातकाल के अवसर पर जब देश के विभिन्न भागों में जनता के साथ ज्यादतियां हुई तो स्व. श्रीमती गांधी के दल (कांग्रेस आई) के ही कुछ सदस्यों ने असन्तोष प्रकट करते हुए श्रीमती गाँधी के इस कदम की न केवल आलोचना ही कि बल्कि अपने अपने पदों से त्यागतत्र भी दे दिये । १९८९ से लेकर वर्तमान तक ऐसे अनेक अवसर आये जब संसद सदस्यों ने अपने विवेक और अन्तरात्मा के अनुसार कार्य किया है, न कि दलीय नेता के इशारे पर । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि गाँधीजी संसदीय लोकतंत्र के विरोधी हैं। वे लाकतंत्र के जिस रूप का सर्मथन करते हैं वह आदर्श लोकतंत्र है। ऐसा आर्दश लोकतंत्र जो सभी आभावों व हिंसा से पूर्ण मुक्त हो, अपने आर्दश लोकतंत्र में वे राजनीतिक अधिकारों, आथ्र्ाक समानता तथा सुरक्षा को अत्यधिक महत्व देते हैं किन्तु इस पर भी वे इनको लोकतंत्र का मूल तत्त्व स्वीकार नहीं करते थे। वे इनको लोकतंत्र का केवल बाह्य ढांचा प्रतीक ही समझते थे। उनके मतानुसार कोई भी समाज लोकतंत्र का सुखभोग केवल उसी सीमा तक कर सकता है जहां तक कि उसके सदस्यों को आन्तरिक स्वतंत्रता अथवा अपनी इच्छाओं तथा भावनाओं को विवेक के अनुसार नियन्त्रित करने की क्षमता प्राप्त होती है। यह आन्तरिक स्वतंत्रता भीतर से विकसित होती है, इसे बाहर से थोपा नहीं जा सकता। इसलिये लोकतंत्र की भावना भी भीतर से विकसित होती है, इसे वयस्क मताधिकार, चुनाव तथा संसद जैसे बाह्य संस्थाओं द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता । उनके अनुसार पश्चिम में लोकतन्त्र की विफलता का कारण वहां पूंजी वाद व उसक यन्त्रों में कुछ दोषों का होना नही ंथा बल्कि उसका वास्तविक कारण यह भी था कि जनगण अपने भीतर आन्तरिक स्वतंत्रता को विकसित नहीं कर पाये। उनका विश्वास था कि जिस समाज के सदस्यों में आन्तरिक स्वराज्य की भावना उत्पन्न नहीं हो जाती वे एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते । आज के सन्दर्भ मे गाँधी के उपर्युक्त विचार सत्य प्रतीत होते हैं। निःसन्देह थोपा गया लोकतंत्र कभी भी स्थायी और सफल नहीं हो सकता । जब तक जनता स्वयं लोकतान्त्रिक भावना की आत्मानुभूति नहीं कर लेती, लेाकतंत्र केा प्रबल समर्थन नहीं मिल सकता। केवल निर्वाचन में खडा होने या मत देने के अधिकार से ही लोकतंत्र की सफलता को मापा नहीं जा सकता। अक्सर निर्वाचन के समय मतदाताओं की उदासीनता देखी गई है,
यह आम धारणा है कि विश्व में सर्वप्रथम राजतंत्र का जन्म हुआ है और उसका विकसित रूप लोकतंत्र है। किन्तु भारतीय साहित्य और राजनीति में इसके विपरीत प्रमाण मिलते हैं, जिसके अनुसार भारत में सर्वप्रथम लोकतंत्र का जन्म हुआ और राजतंत्र उसका विकृत रूप है। भारत में राजनीतिक विचारधारा देशकाल से प्रभावित होकर पाश्चात्य विचारधारा से बहुत कुछ भिन्न रही है। यद्यपि भारतीय साहित्य में लोकतंत्र में रूचि नहीं रखते थे। वास्तव में उनकी दृष्टि से लोकतंत्र और धर्म मर्यादित राजतंत्र में अधिक अन्तर नहीं था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब लोकतंत्र पर बहस होती है तो उत्तरदायी लोकतंत्र अर्थात संसदीय लोकतंत्र उभर कर हमारे सामने आता है। जिसे यदि सीमित बहुसंख्यक जनता का शासन भी कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा । बहुदलीय प्रणाली, राजनीतिक दल-बदलद्व स्पष्ट बहुमत का आभाव आदि अनेक दोषों से ग्रसित संसदीय लोकतंत्र की सफलता पर विद्वानों में पर्याप्त बहस होने लगी है। भारत के संदर्भ में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी लोकतन्त्र के पक्षधर होते हुए भी संसदीय लोकतन्त्र के प्रति अपनी आपत्तियां रखते है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि गांधीजी के राजनीतिक विचारों में लोकतंत्र के प्रति उनकी निष्ठा सर्वत्र विद्यमान है। किन्तु उन्होंने लोकतंत्र के सामाजिक उत्थान के पक्ष को महत्व दिया है। वे अभिजातीय लोकतंत्र तथा पंचवर्षीय मतदान की प्रणाली वाले औपचारिक लोकतंत्र के पक्ष मे नहीं है। उनके लोकतंत्र में एक ओर समाज के दलित वर्गो द्वारा कुलीन तथा पूंजीपति वर्गो के नियन्त्रण के विरूद्व राजनीतिक आन्दोलन की प्रेरणा मिलती है तो दूसरी ओर ऐसे आर्दश समाज की मांग, जिसमें व्यक्ति को स्वशासन का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके । गाँधीजी के सर्वोदयी उदारवादी लोकतंत्र में दलविहीन राजनीति के दर्शन होते हैं। गाँधीजी सर्वोदय तथा अंत्योदय की दृष्टि से ऐसे समतावादी समाज के समर्थक हैं जिसमें नेता तथा जनता एक ही धरातल पर सादगी एवं संयम से जनसेवा का कार्य करते रहें। वे लोकतंत्र को ''मिलावटविहिन अहिंसा का शासन'' मानते हैं। लोकतंत्र अर्थात् अहिंसा, व्यक्ति की आत्मशुद्वि या नैतिक उत्थान को लिए हुए हैं। राजनीतिक स्वशासन जिसमें अनेक पुरूषों तथा स्त्रियों का स्वाशासन अन्तर्निहित है। व्यक्तिगत स्वशासन से बढकर नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि गाँधीजी को इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि व्यक्तिगत स्वशासन वह शासन है, जो न केवल सामाजिक मूल्यों वरन् व्यक्ति की गरिमा को भी बनाये रखने में सहायक है। गाँधीजी पाश्चात्य देशों के लोकतान्त्रिक उदाहरणों से सन्तुष्ट नहीं है, क्योंकि वहां शस्त्रास्त्र की होड, साम्रज्यबाद, शोषण, पूंजीवाद, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा नेतृत्व के अभाव ने सच्चे लोकतान्त्रिक मूल्यों को भुला दिया है। राज्य का आर्थिक कार्यों में हस्तक्षेप, राज्य शक्ति के बढते हुए दायरे का प्रतीक बन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निगलने के लिये मुँह बाएँ खडा है। ऐसे भयावह राज्य से मुक्ति प्राप्त करने के लिये उचित नियंत्रण तथा सन्तुलन ढूंढने की आवश्यकता हैं। गाँधीजी के विचारों से स्पष्ट होता है कि उनकी नजर में लोकतंत्र समाज के सभी वर्गो के समस्त भौतिक और आध्यात्मिक साधनों को सबकी भलाई के लिये संगठित करने की कला और विज्ञान हैं। उनका मानना है कि लोकतंत्र वह है जिसमें दुर्बल और सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हों लेकिन वे यह भी मानते है कि विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं हैं। गाँधीजी के चिन्तन में लोकतंत्र के प्रति स्वाभाविक निष्ठा प्रकट होती है क्योंकि उनकी विचारधारा में व्यक्ति को जो सम्मान प्राप्त है, वही लोकतंत्र का भी आधार है। सार यह है कि व्यक्ति का सर्वोच्च एवं सर्वागींण विकास गाँधीजी के चिन्तन में प्रमुख स्थान रखता है। यदि लोकतंत्र, शासन अथवा जीवन की वह पद्वति है जो समाज के सभी व्यक्तियों को समानता के धरातल पर संगठित कर उन्हें उनकी सर्वोच्च मंजिल तक पहुँचाती है तो गाँधीजी को यह अत्यन्त प्रिय है लेकिन पश्चिमी प्रजातंत्र अथव संसदीय प्रणाली ऐसा करने में सर्वथा असमर्थ है इसलिए गाँधीजी इसके समर्थक नहीं है। गाँधीजी ने पाश्चात्य राज्य पद्धतियों की आलोचना की । अन्य राज्य पद्धतियां तो दोषपूर्ण पहले से ही मानी जाती थी, परन्तु संसदीय लोकतन्त्र जो सभी राज्य पद्धतियों में निर्दोष माना जाता है तथा मानव-कल्याण और हित का दावा करता है। उनके मत में वह भी दोषपूर्ण है और हिंसा पर आधारित है, इससे मानव का सच्चा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होनें प्रचलित संसदीय लोकतंत्र में अविश्वास व्यक्त किया। लोकतंत्र जिस रूप में पश्चिम में स्वीकृत है उससे वे सहमत नहीं थे। संसदीय लोकतंत्र की उनकी आलोचना का मुख्य आधार यह था कि उसमें ईमानदारी और जन-कल्याण की भावना से बहुत कम काम होता है और ढग तथा प्रदर्शन का अधिक। गाँधीजी का कहना था कि अहिंसा और नैतिक शुद्धता में विश्वास न होने के कारण पश्चिम के राज्यों में नाममात्र का लोकतंत्र है, उनमें लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रति वास्तविक लगाव नहीं पाया जाता है। गाँधीजी प्रेम को लोकतंत्र का सच्चा आधार मानते है, उनके विचार में प्रेम लोकतंत्र के विकास में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसके अलावा स्वयं व्यक्ति का अच्छा होना, अहिंसा व नैतिकता के नियमों का पालन आदि को भी वे लोकतंत्र के विकास में सहायक मानते हैं। गाँधीजी के इन विचारों से उन लोगों को छोडकर जिन्हें लोकतन्त्रिय शासन में विश्वास नहीं है, शायद ही कोई इन्कार कर सकता है। गाँधीजी के विचारों से यह भी स्पष्ट होता है कि पश्चिम में लोकतत्र के सफल न हो सकने का कारण संस्थाओं की पूर्णता उतनी ही है, जितनी सिद्धान्तों की अपूर्णता है। विशेष रूप से हिंसा और असत्य की उपयोगिता म विश्वास । लोकतंत्र उन गलत विचारों और आदर्शो से विकृत होता हैं। जो मनुष्यों का संचालन करते हैं यदि जनता ने शुद्ध अहिंसा के मार्ग को अपनाया तो लोकतंत्रवादी राज्य के ये दोष बहुत कम हो जायेंगे। गाँधीजी ने विश्वास प्रकट किया कि लोकतंत्र का विकास, बल प्रयोग से नहीं हो सकता । लोकतंत्र की सच्ची भावना बहार से नहीं अपितु भीतर से उत्पन्न होती है। कानून पास करने से बुराइयां दूर नहीं की जा सकती, मूल बात तो यह है कि हृदय को बदला जाये । यदि हृदय बदले बिना व्यवस्थापन कर दिया जाये तो महत्वहीन होगा । कानून सदैव आत्मरक्षा के लिये बनाये जाने चाहिए यदि वे उन्नति और विकास को रोकते हैं तो वे बेकार हैं, कोई भी मानवीय कानून स्थायी रूप से व्यक्ति के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकते। गाँधीजी की पुस्तक ''हिन्द-स्वराज्य'' के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वे संसदीय लोकतंत्र के पक्ष में नही थें । उनके मत में - ''जिसे आप पार्लियामेंट की मॉ'' कहते है, वह तो बांझ और वैश्या है। ये दोनों शब्द कठोर हैं पर उस पर पूरी तरह चरिर्ताथ होते है। उसे बांझ मैं इसलिए कहता हूं कि अब तक उसने एक भी अच्छा काम अपने आप नहीं किया। उसकी स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति है कि उसके ऊपर दबाव देने वाला कोई न कोई हो तो वह कुछ भी न करे और वैश्या वह इसलिए है कि जो मन्त्रीमण्डल वह बनाती है उसके वश में रहती है।'' इसके अलावा उसका कोई एक मालिक मुख्तार भी नहीं है। उसका मुखिया कोई एक आदमी हो ही नहीं सकता। उसका मुखिया जब कोई बनता है जैसे कि प्रधानमंत्री, तब भी उसकी चाल एक सी नही रहती। जो दुर्गति वैश्या की होती है वही सदा उसकी रहती है। प्रधानमन्त्री को संसद की चिन्ता अधिक नहीं होती, वह तो अपनी शक्ति के मद में चूर रहता है, उसका पक्ष कैसे जीते इसी की चिन्ता उसे रहती है। संसद ठीक काम कैसे करे इसकी फिक्र उसे ज्यादा नहीं होती। अपने पक्ष का बल बढाने के लिए वह संसद से कैसे कैसे काम करवाता है। गाँाधीजी के से विचार आज के सन्दर्भ में पूर्णतया सत्य प्रतीत होते हैं। प्रायः देखा गया है कि संसदीय प्रजातंत्र में दलगत राजनीति कार्य करती है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं परन्तु वास्तव में उसकी कर्त्तव्यनिष्ठा अपने परिवार या अपनी पार्टी तक ही सीमित रहती है। जनता के कल्याण के लिए वे कुछ भी नहीं कर पाते । जो जिस दल का सदस्य होता है उसी को आँख मूंद कर वोट कर देता है, अथवा देने को मजबूर है। कोई इस नियम का अपवाद बन जाए तो समझ लीजिए कि उसकी सदस्यता के दिन पूरे हो गए। जितना समय और पैसा संसद बरबाद करती है उतना समय और पैसा थोडे से भले आदमियों को सौंप दिया जाय तो उद्वार हो जाय । एक ब्रिटिस संसद सदस्य ने तो यहां तक कह दिया कि संसद इस लायक नहीं रही कि कोई सच्चा ईसाई उसका सदस्य हो सके। एक अन्य सदस्य का कहना था कि संसद तो अभी दूध पीती बच्ची हैं । इस पर बच्चा सदा बच्चा ही बना रहे ये बात क्या आपने देखी है। सात सौ साल हो जाने पर भी संसद बच्ची ही बनी है तो सयानी कब होगी? इसी कारण संसद में बहुत अधिक अस्थिरता पाई जाती है और यही करण है कि उसके फैसलों में कोई पक्कापन नहीं होता । आज का फैसला कल रद्द कर दिया जाता है। सम्भवतः एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि संसद ने कोई काम करके उसे अन्त तक पहुंचाया हो । यही नहीं संसद क सदस्य महत्वपूण्र्ा और बडे मसलों पर विवाद के समय बैठे-बैठे ऊंधा करते है, कभी संसद में वे इतना शोर मचाते हैं कि सुनने वालों की हिम्मत टूट जाती है। भारत की संसद में तो अनेक बार संसद सदस्यों द्वारा गाली-गलौंच छीना-झपटी, एक दूसरे के कपडे फाड देना, माईक व पेपरवेट फेंकना, टेबल उलट देना जैसी घटनाएं देखी गई हैं। जिससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। क्या यही वे सदस्य हैं जो सरकार में हमारे प्रतिनिधी हैं? संक्षेप में संसद न तो किसी के प्रति वफादार होती है और न उसमें सृजन की क्षमता ही होती है। इसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया । गांधीजी के मत में ब्रिटिश प्रजातंत्र में समस्त जनता के कल्याण का भार कुछ चुने हुए प्रतिनिधि ले लेते हैं। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी हाथ नहीं बंटा पाती है। सम्पूर्ण जनता वास्तव में अपने कल्याण के लिए राज्य के प्रतिनिधियों की गुलाम हो जाती है, उनका शोषण होता है। अतः गाँधीजी की राय में यह पद्वति हिंसा से पूर्ण है। उसमें नाजीवाद और फांसीवाद उपनिवेशवादी नीति को ढकने का एक बडा आवरण है। इसकी सभी संस्थाएं अलोकतांत्रिक तथा हिंसा से पूर्ण है। अतः ब्रिटिश लोकतंत्र उपयोगी पद्वति नहीं है। गांधीजी का यह मत कुछ अंशो में सत्य माना जा सकता है। यह सत्य है कि संसद के सदस्य कठोर दलीय अनुशासन में बन्धें होते हैं और उनका सम्पूर्ण व्यहवार अपने अपने दल के नेता के इशारे द्वारा निर्धारित होता है किन्तु गाँधीजी की इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि संसद ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया । भले ही संसद के सदस्य ने जनभावनाओं को अभिव्यक्त कर उसकी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा की है। यह कहना भी सत्य नहीं है कि संसद के सदस्य दलगत राजनीति से प्रेरित और सदैव दलीय नेता के इशारे पर कार्य करते रहे है। ब्रिटेन और भारत में ऐसे अनेक अवसर आये हैं जब संसद के सदस्यों ने दलीय राजनीति से प्रेरित होकर नहीं बल्कि अपने विवेक और अन्तरात्मा की आवाज के आधार पर कार्य किया है। १९७५ में प्रधानमन्त्री स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा लगाये गए आपातकाल के अवसर पर जब देश के विभिन्न भागों में जनता के साथ ज्यादतियां हुई तो स्व. श्रीमती गांधी के दल (कांग्रेस आई) के ही कुछ सदस्यों ने असन्तोष प्रकट करते हुए श्रीमती गाँधी के इस कदम की न केवल आलोचना ही कि बल्कि अपने अपने पदों से त्यागतत्र भी दे दिये । १९८९ से लेकर वर्तमान तक ऐसे अनेक अवसर आये जब संसद सदस्यों ने अपने विवेक और अन्तरात्मा के अनुसार कार्य किया है, न कि दलीय नेता के इशारे पर । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि गाँधीजी संसदीय लोकतंत्र के विरोधी हैं। वे लाकतंत्र के जिस रूप का सर्मथन करते हैं वह आदर्श लोकतंत्र है। ऐसा आर्दश लोकतंत्र जो सभी आभावों व हिंसा से पूर्ण मुक्त हो, अपने आर्दश लोकतंत्र में वे राजनीतिक अधिकारों, आथ्र्ाक समानता तथा सुरक्षा को अत्यधिक महत्व देते हैं किन्तु इस पर भी वे इनको लोकतंत्र का मूल तत्त्व स्वीकार नहीं करते थे। वे इनको लोकतंत्र का केवल बाह्य ढांचा प्रतीक ही समझते थे। उनके मतानुसार कोई भी समाज लोकतंत्र का सुखभोग केवल उसी सीमा तक कर सकता है जहां तक कि उसके सदस्यों को आन्तरिक स्वतंत्रता अथवा अपनी इच्छाओं तथा भावनाओं को विवेक के अनुसार नियन्त्रित करने की क्षमता प्राप्त होती है। यह आन्तरिक स्वतंत्रता भीतर से विकसित होती है, इसे बाहर से थोपा नहीं जा सकता। इसलिये लोकतंत्र की भावना भी भीतर से विकसित होती है, इसे वयस्क मताधिकार, चुनाव तथा संसद जैसे बाह्य संस्थाओं द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता । उनके अनुसार पश्चिम में लोकतन्त्र की विफलता का कारण वहां पूंजी वाद व उसक यन्त्रों में कुछ दोषों का होना नही ंथा बल्कि उसका वास्तविक कारण यह भी था कि जनगण अपने भीतर आन्तरिक स्वतंत्रता को विकसित नहीं कर पाये। उनका विश्वास था कि जिस समाज के सदस्यों में आन्तरिक स्वराज्य की भावना उत्पन्न नहीं हो जाती वे एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते । आज के सन्दर्भ मे गाँधी के उपर्युक्त विचार सत्य प्रतीत होते हैं। निःसन्देह थोपा गया लोकतंत्र कभी भी स्थायी और सफल नहीं हो सकता । जब तक जनता स्वयं लोकतान्त्रिक भावना की आत्मानुभूति नहीं कर लेती, लेाकतंत्र केा प्रबल समर्थन नहीं मिल सकता। केवल निर्वाचन में खडा होने या मत देने के अधिकार से ही लोकतंत्र की सफलता को मापा नहीं जा सकता। अक्सर निर्वाचन के समय मतदाताओं की उदासीनता देखी गई है,http://www.khabarexpress.com/Mahamta-Gandhi-ke-Sansadiya-Loktantra-Vicharo-ki-Vartmaan-me-prasangita.-article_74.html
 महिला आरक्षण बिल के पहले वैधानिक दौर के बाद विजेता स्वयं को हतप्रभ और पराजित विचलित पा रहे हैं। लेकिन पटकथा में ऐसा नहीं था। जब सारे दिग्गज लैंगिक भेदभाव में सुधार के हक में हों, जिनमें मीडिया जैसा सबसे बड़ा दिग्गज भी शामिल हो, तब इस लड़ाई का अंत पुरातनपंथियों के एक पूरे जत्थे के खिलाफ आसान जीत के साथ ही होना था।
महिला आरक्षण बिल के पहले वैधानिक दौर के बाद विजेता स्वयं को हतप्रभ और पराजित विचलित पा रहे हैं। लेकिन पटकथा में ऐसा नहीं था। जब सारे दिग्गज लैंगिक भेदभाव में सुधार के हक में हों, जिनमें मीडिया जैसा सबसे बड़ा दिग्गज भी शामिल हो, तब इस लड़ाई का अंत पुरातनपंथियों के एक पूरे जत्थे के खिलाफ आसान जीत के साथ ही होना था।
सच है कि राज्यसभा में वोटिंग के बाद स्कोर इस तरह था: श्रीमती सोनिया सुषमा ब्रिंदा गोलिएथ 1 और श्री यादव खान डेविड 0। लेकिन गोलिएथ खेमा लोकसभा के अगले मैच में अपनी संभावनाओं को लेकर अधिक चिंतित हो गया, जबकि डेविड खेमा अपनी गुलेल को मजे से चमका रहा है। आत्मविश्वास से भरी श्रीमती गोलिएथ से अपेक्षा की जा रही थी कि वे इस पूर्वानुमान पर जोरदार वापसी करेंगी कि डेविड गुट मुसीबत में है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फैसले को स्थगित कर दिया गया।
यहां यह नहीं सुझाया जा रहा है कि श्रीमती गोलिएथ मैच हारने की स्थिति में हैं। लेकिन यह तो निर्विवाद ही है कि एक दुर्जेय किले में सेंध जरूर लग चुकी है। जिस विजयी मुद्रा के साथ उन्होंने मैच की शुरुआत की थी और जो संविधान में 108 वें संशोधन तक जारी रही, उसकी जगह गहरी असहजता ने ले ली है। यह इसलिए है कि दिल्ली की मुस्कराहटें जमीनी संवेदनाओं और खासतौर पर उत्तरी भारत की संवेदनाओं से मेल नहीं खातीं। बिल का विरोध कर रहे नेता भारतीय समाज के वंचित तबकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें दलित, पिछड़े व मुस्लिम शामिल हैं। आम आदमी के हितों को सामने रखने का दावा करने वाली सरकार निश्चित ही इससे चिंतित है कि वह 'खास औरत' की आवाज के रूप में तब्दील हो जाएगी।
इस तमाम बखेड़े के पीछे एक वाजिब सवाल है: क्या यह आरक्षण किन्हीं खास महिलाओं के लिए है या सभी महिलाओं के लिए है? न तो पुरुष और न ही महिलाएं सजातीय समूह हैं और न ही महिला या पुरुष होना किसी की राजनीतिक पहचान हो सकती है। यदि महिलाओं को महिलाओं के लिए ही मतदान करना होता तो वर्तमान लोकसभा महिलाओं से भरी पड़ी होती, क्योंकि हर दूसरा मतदाता एक महिला है। पार्टियां ज्यादा महिला उम्मीदवारों का चयन नहीं करतीं, इसका लैंगिक पक्षपात से कोई लेना-देना नहीं है। यह इसलिए है, क्योंकि चुनावी राजनीति में महिलाओं को बहुत से नुकसान उठाने पड़ते हैं, जिससे उनके लिए पुरुष उम्मीदवारों को हराना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आरक्षण के जरिए सदन में उनकी संख्या बढ़ाने का यह एक तार्किक औचित्य है। लेकिन यदि आरक्षण पुरुषों व महिलाओं के बीच के असंतुलन को कम करने के लिए आवश्यक है तो इसी तर्क के साथ यह भी आवश्यक है कि महिलाओं और महिलाओं के बीच के असंतुलन को कम किया जाए। संपत्ति, जाति और धर्म इस आंतरिक असंतुलन के निर्णायक तत्व हैं और आरक्षण के भीतर आरक्षण एक विवेकपूर्ण बात होगी। जो ये तर्क देते हैं कि धर्म आधारित आरक्षण को संवैधानिक स्वीकृति नहीं है, वे भूल जाते हैं कि यह मामूली बिल नहीं, संवैधानिक संशोधन है। यदि आप एक कारण से संविधान में संशोधन कर सकते हैं तो किसी दूसरे कारण से भी कर सकते हैं।
लोकसभा में अगर जनप्रतिनिधियों का अनुपात सही नहीं होगा तो वह सही काम भी नहीं कर पाएगी। लिहाजा सुधार आवश्यक हैं। कुछ सुधार सरल होते हैं, जैसे हर आम चुनाव में बारी-बारी से सीटों के आरक्षण की रोटेशन प्रणाली का प्रस्ताव, जिसका विफल होना तय है। इस पर आसानी से दो-तिहाई लोकसभा सांसदों का अगला कार्यकाल अनिश्चित होगा। जिससे इन सांसदों और मतदाताओं के बीच जवाबदेही का रिश्ता समाप्त हो जाएगा। लेकिन संसदीय प्रणाली की अधिक घातक सच्चइयां परदे के पीछे छिपी हैं। इनमें सर्वाधिक खतरनाक यह है कि भारतीय संसद धनाढच्यों की आश्रयस्थली बन चुकी है। नेशनल इलेक्शन वॉच बताता है कि वर्तमान लोकसभा में 59 महिलाएं हैं, जो मुस्लिमों की संख्या से लगभग दुगुनी है। पिछले छह दशकों से जहां महिला सांसदों की संख्या बढ़ी है, वहीं मुस्लिमों की संख्या घटी है। 59 में से 40 महिला सांसदों यानी 68 प्रतिशत की निजी संपत्ति एक करोड़ रुपए से अधिक है। धनाढच्य पुरुष सांसदों का प्रतिशत (57 प्रतिशत) इससे बहुत अलग नहीं है। ये सभी अपनी संपत्ति छिपाते हैं। हमारी संसद एक एलीट क्लब बन चुकी है। चुनाव की लागतें देखें तो साधनहीन व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना लगभग असंभव ही है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वालों के लिए आखिर कोई आरक्षण की मांग क्यों नहीं करता। सही मायनों में क्रांति तो वही होगी।
http://www.bhaskar.com/2010/03/14/100314004755_special_woman.html
विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां : शोषण की नयी कहानी
सीएससी की भारतीय शाखाओं में मोहल्ला लाइव पर बैन

नोएडा में मौजूद सीएससी इंडिया प्रा लि के दफ्तर की तस्वीर
अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब किसी भारतीय को अपने ही देश में आने के लिए, हवाई जहाज के टायलेट में घुसकर आने का खतरा उठाना पडता है तो स्थिति कितनी भयावह होगी। यह सब 9/11 के बाद तो किसी आम आदमी के लिए असंभव ही लगता है। अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए अरब देश जाने का सपना संजोये लोगों के लिए यह घटना आंखें खोलने वाली थी। डाइनिंग हाल में अपने अपने टीवी सेट पर इस खबर को देखकर हममें से कइयों ने ऐसी शोषणपूर्ण स्थिति पर अफसोस जताया था। लेकिन हम भूल गये थे कि कम से कम नीली कॉलर वालों ने यूनियन बनाना सीख लिया है। मांगें मानी जाए या नहीं, लेकिन अपने हकों के बारे में कम से कम कभी-कभी बोलना तो सीख लिया है। एसी गाड़ियों में ऑफिस जाते जाते हम भूल से जाते हैं कि फिर लौटकर मुनीरका जैसी गलियों में ही आना है।
इकनॉमिक टाइम्स में कल एक खबर छपी – डेनमार्क में भारतीय आईटी पेशेवरों के शोषण के लिए CSC India Pvt Ltd जांच के घेरे में।
डेनमार्क के कानून के तहत, बाहर से आये पेशेवरों को कम से कम 31,250 क्रोनर (डेनमार्क मुद्रा) देना जरूरी है जबकि CSC पांच से आठ हजार क्रोनर ही देती आ रही थी। इस मुद्दे को वहां के आईटी पेशेवरों के यूनियन ने उठाया तब से यह कंपनी पसोपेश में है। यहां काम करते हुए यह तो कहा ही जा सकता है कि यह कंपनी केवल डेनमार्क में ही नहीं, हर जगह सबसे कम वेतन देने के लिए बदनाम रही है। भारत में भी यह अपवाद नहीं है। नोएडा में जहां कंपनी का मुख्यालय है, करीब दस हजार लोग काम कर रहे हैं। चयन के वक्त जितना कहा जा सके, उतने आश्वासन दिये जाते हैं जबकि असलियत पहली सैलरी के बाद समझ में आती है। वास्तविक सैलरी सकल आय से 30-40% कम आती है। फिर शुरू होता है स्पष्टीकरण का सिलसिला।
क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसी गाड़ियों में रात के वक्त ऑफिस जाने वाले की कुल आमदनी महज सात हजार रुपये होगी? जीने के लिए तो लोग तीन हजार की नौकरियां करके जी रहे हैं लेकिन क्या भारत सरकार, जो जब तब एस्मा और पता नहीं कितने सारे कानून लाती रहती है, उसके लिए यह सब नियम के विरुद्ध नहीं लगता? हर अगले सप्ताह किसी न किसी का ई-मेल आता रहता है, जिसमें कभी 20% सकल लाभ तो कभी नयी नयी बिजनेस उप्लब्धियों को गिनाया गया होता है। जबकि सच यह है कि पिछले दो साल से किसी भी कर्मचारी की सैलरी बढ़ी तो नहीं लेकिन घट जरूर गयी है। लिहाजा लोग अपने खर्चों में कटौती करके किसी दूसरे विकल्प का इंतजार कर रहे हैं।
बेसिक सैलरी की वजह से बोनस न देना पड़े, इस वजह से इस कंपनी ने पूरी की पूरी सकल सैलरी को बेसिक बना दिया है। लिहाजा 24% सैलरी तो पीएफ में ही कट जाती है क्योंकि प्रोविडेंट फंड में कंपनी के योगदान को भी दिखा कर यह कंपनी एक ऊंची सैलरी देने का ढोंग करती है। दो साल से काम कर रहे लोगों को कभी इस जनवरी में तो कभी अगले जुलाई में प्रोमोट करने का लालच देती रहती है।
आगामी एक अप्रेल से लंच में कंपनी की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी भी बंद की जा रही है। लिहाजा अब सभी को कम से कम एक समय के लिए पचास रुपये खाने पर देने होंगे। वो भी सात हजार की सैलरी में से।
इन सब गतिविधियों के मद्देनजर कम से कम पिछले छह महीनों में ही दो हजार से ज्यादा लोगों ने कंपनी छोड़ दी है और दूसरों ने अपने लिए दूसरे विकल्प तलाशने शुरू कर दिये हैं। लेकिन कंपनी एक नया नियम ले कर आयी है, जिससे लगता है कि भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों को बंधुआ मजदूरी करवाने के अधिकार भी दे दिये हैं? नये नियम के अनुसार अब हर किसी के लिए दो महीने का नोटिस देना होगा। न तो इन दो महीनों को छुट्टियों से कम किया जाएगा, न ही हम पैसे देकर इन दो महीनों से बच सकते हैं। इसका साफ मतलब है कि न ही कोई दूसरी कंपनी दो महीने के लिए रुकेगी, न ही हम इस कंपनी को छोड़ पाएंगे।
सवाल यह है कि क्या कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को इस तरह मजबूर कर सकती है? क्या पता कि किसी दूसरी कंपनी में भी ऐसे ही नियम-कायदे हों? क्या हम बस इन कंपनियों की दया के ही भरोसे रह गये हैं। कोई तो नियम कायदा होगा, जो हमारे हितों की रक्षा करता हो? ऐसे कौन से नियम हैं, जिनका फायदा उठा कर कोई इतनी बड़ी कंपनी महज सात हजार रुपये देकर अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ लेती है। ऐसी कौन सी सर्वे कंपनी है, जो ऐसी कंपनियों को बेस्ट फाइव और बेस्ट टेन में घोषित करती है। यह लिखने का एक दूसरा और सीधा मकसद यह भी है कि लोग समझें कि बड़ी-बड़ी कंपनियों में सब कुछ अच्छा ही नहीं होता। ऊंची दुकान और फीकी पकवान CSC के लिए भी सही कहा जा सकता है।
http://mohallalive.com/2010/03/30/the-position-of-foreign-corporate-companies-in-our-country/♦ एक कर्मचारी
Articles tagged with: dilip mandal
ख़बर भी नज़र भी, नज़रिया »

दिलीप मंडल ♦ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती की माला को लेकर राजनीति और भद्र समाज में मचा शोर अकारण है। मायावती ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो वतर्मान राजनीतिक संस्कृति और परंपरा के विपरीत है। नेताओं को सोने-चांदी से तौलने और रुपयों का हार पहनाने को लेकर ऐसा शोर पहले कभी नहीं मचा। नेताओं की आर्थिक हैसियत के खुलेआम प्रदर्शन का यह कोई अकेला मामला नहीं है। सड़क मार्ग से दो घंटे में पहुंचना संभव होने के बावजूद जब बड़े नेता हेलिकॉप्टर से सभा के लिए पहुंचते हैं, तो किसी को शिकायत नहीं होती। करोड़ों रुपये से लड़े जा रहे चुनाव के बारे में देश और समाज अभ्यस्त हो चुका है।
ख़बर भी नज़र भी, नज़रिया »

वेदप्रताप वैदिक ♦ आरक्षण में आरक्षण के बिना यह आरक्षण अधूरा है, क्योंकि लगभग सभी महिला सीटों पर ऊंची जातियों की महिलाओं का कब्जा हो जाएगा। यह तर्क तथ्यात्मक तो है, पर आरक्षण में यदि आरक्षण दे भी दिया गया होता, तो क्या होता? कठपुतलीवाद बढता, राबड़ीवाद दन्नाता। सर्वथा अयोग्य महिलाओं को पकड़ कर गद्दी पर बैठा दिया जाता। वे क्या खाक कानून बनातीं? वे अपने पार्टी-नेताओं के इशारों पर ही निर्णय लेतीं। यानी, संसद का मजाक बनता। अभी तो प्रयत्न यह होना चाहिए कि सक्षम महिलाओं को ही संसद में भेजा जाए, जो महिला उत्थान के बारे में खुद सोच सकें और जरूरत पडने पर पुरुषों को बराबरी की टक्कर दे सकें।
ख़बर भी नज़र भी, नज़रिया »

दिलीप मंडल ♦ अगर कहूंगा कि ये सभी महिलाएं (ऊपर की तस्वीर में दोनों – सुषमा और वृंदा जी और नीचे की तस्वीर में चारों – सुषमा, वृंदा, नजमा और माया जी) किस क्लास या कास्ट से हैं, तो आप कहेंगे कि जातिवाद फैला रहा हूं। इस शहर में कुछ है जो सड़ रहा है! भारत के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दुनिया में 134वें नंबर पर होने के कारणों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहा हूं।
ख़बर भी नज़र भी, नज़रिया »

अच्छी फिल्म, बुरे दर्शक
मधुकर पांडेय ♦ इस बेहतरीन फिल्म के साथ जैसा दुर्व्यवहार हो रहा है, वह अफसोसनाक है। मेरे हिसाब से इस फिल्म को पूरे देश में करमुक्त कर देना चाहिए।
दून में शब्द मेला
डेस्क ♦ देहरादून में यात्रा, पेंग्विन और दून लाइब्रेरी मिल कर अप्रैल के पहले हफ्ते में एक साहित्य मेला लगाने जा रहा है, जिसमें शब्दजीवियों का जमघट लगेगा।
ख़बर भी नज़र भी, नज़रिया, बात मुलाक़ात »

विभूति नारायण राय ♦ उस दिन जो जुलूस निकला, उसमें जातिवादी नारे लगाये गये। हमारा जो कर्मचारी संघ का अध्यक्ष है, वो बड़ा उत्तेजित हो कर आया। वो ब्राह्मण है। उसने कहा कि देखिए ये मां-बहन की गालियां दे रहे हैं। तो मैंने कारुण्यकारा से कहा कि भई आप प्रोफेसर हो… ऐसा स्टूडेंट या बाहर के एलिमेंट आकर कर रहे थे तो समझ में आता है… लेकिन आप प्रोफेसर हो और आप भी इसमें शरीक हो गये? ये मैंने एक तरह से उनको वार्न किया कि भविष्य में जहां इस तरह के प्रोवोकेटिव नारे लगाये जाएं, तो वहां किसी प्रोफेसर को नहीं जाना चाहिए।
ख़बर भी नज़र भी, नज़रिया, बात मुलाक़ात, मीडिया मंडी »

विभूति नारायण राय ♦ आपको यह तथ्य नहीं मालूम है कि नागपुर में हाईकोर्ट में अनिल चमड़िया के ख़िलाफ़ एक रिट है। एक सज्जन जो कि… आशुतोष मिश्रा नाम के एक सज्जन हैं, जो उसी इंटरव्यू में आये थे, जिनका सलेक्शन नहीं हुआ था। तो आशुतोष मिश्रा ने एक रिट कर रखी है हाईकोर्ट में। उन्होंने कहा है कि भाई साहब 2002 या फिर 2001… अब आप कह रहे हैं कि 2000 तो यूजीसी की 2000 वाली गाइडलाइंस का यूनिवर्सिटी ने उल्लंघन किया है। यह विश्वविद्यालय को अधिकार नहीं था। यह ईसी के बैठक से पहले की बात है। हफ़्ते-दस दिन पहले की बात। जब हमने अपना पक्ष रखा, तो हमने स्वीकार कर लिया था कि हमसे ग़लती हो गयी थी। और हम इस ग़लती को सुधार कर आपके पास आएंगे।
ख़बर भी नज़र भी, नज़रिया, समाचार »

दिलीप मंडल ♦ जब वर्धा में प्रोफेसर अनिल चमड़िया की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश जारी किया जा रहा था, लगभग उन्हीं दिनों दूर दक्षिण में मैंगलोर यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही एक फैसला हो रहा था। एक यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार की है और दूसरी यूनिवर्सिटी एक ऐसे राज्य में चल रही है, जहां बीजेपी का शासन है। एक यूनिवर्सिटी को तथाकथित प्रगतिशील का गौरवशाली नेतृत्व हासिल है तो दूसरे पर संघ की ध्वजा लहरा रही है। लेकिन जब लोकतांत्रिक आचरण की धज्जियां उड़ाने की बात हो तो दोनों विश्वविद्यालयों में अदभुत समानताएं दिखती हैं।
ख़बर भी नज़र भी, नज़रिया, स्मृति »

दिलीप मंडल ♦ ज्योति बसु पर बात करने वालों की नीयत पर संदेह करने से कोई फायदा नहीं होगा। सीपीएम के हितैषियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यभार है कि वो बताएं कि ज्योति बसु की पहली (1977) और दूसरी (1982) कैबिनेट में कोई दलित या आदिवासी मंत्री शामिल था। सोचकर देखिए। एक कैबिनेट बनायी जाती है, वो भी कैबिनेट उन पार्टियों की, जो देश को बेहतर देश बनाना चाहते हैं और पूरी कैबिनेट में एक भी दलित या आदिवासी मंत्री नहीं। जबकि पश्चिम बंगाल में लगभग 30 फीसदी आबादी दलितों और आदिवासियों की है। अगर ये संयोग है, तो बेहद दुखद और शर्मनाक संयोग है।
ख़बर भी नज़र भी, नज़रिया, स्मृति »

दिलीप मंडल ♦ पश्चिम बंगाल में मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, ड्रॉपआउट रेट राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है, सरकारी नौकरियां उन्हें अमूमन मिलती नहीं हैं, राज्य में ओबीसी आरक्षण इतना कम है कि उन्हें उसमें हिस्सा मुश्किल से मिलता है और निजी रोजगार करने के लिए बैंक लोन मिलना आसान नहीं है। इसे किसी समुदाय के खिलाफ हिंसा की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जा सकता? आश्चर्य इस बात का कि ये सब उस शासन में हुआ और हो रहा है, जो निहायत ही "सेकुलर" है! ऐसे सेकुलरवाद से देश के हर वंचित समुदाय को खतरा है।
ख़बर भी नज़र भी, नज़रिया, स्मृति »

अजीत कुमार ♦ बड़ी बेबसी में हूं। न तो आपकी बातों को पूरी तरह से नकार सकता हूं और न पूरी तरह से स्वीकार कर सकता हूं। जहां तक मरने के बाद विभिन्न नेताओं और उद्योगपतियों की तरफ से आये निर्दोष बयान का मामला है। यह तो हमारे यहां परिपाटी बन चुकी है कि देहांत के तुरंत बाद उस व्यक्ति की आलोचना से एक हद तक बचा जाए। भाजपा के नेताओं की तरफ से भी आलोचना के स्वर न आने के पीछे भी सिर्फ एक परिपाटी का चलन ही है। इसी परिपाटी के चलते ही और भी नेताओं, संगठनों व सम्मानित जनों द्वारा आलोचना से गुरेज किया गया है। खैर इस मौके पर भी आपकी आलोचना से मैं असहमत नहीं हूं। यह तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह परिपाटी का मान या सम्मान करे।
http://mohallalive.com/tag/dilip-mandal/




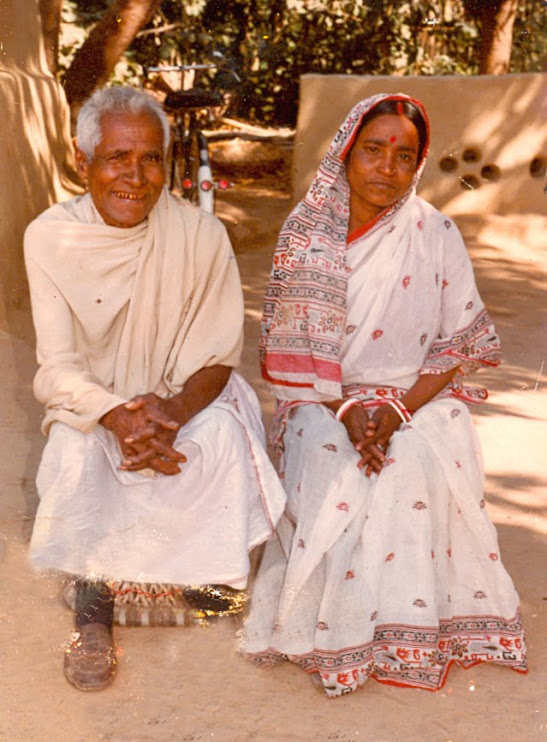



No comments:
Post a Comment